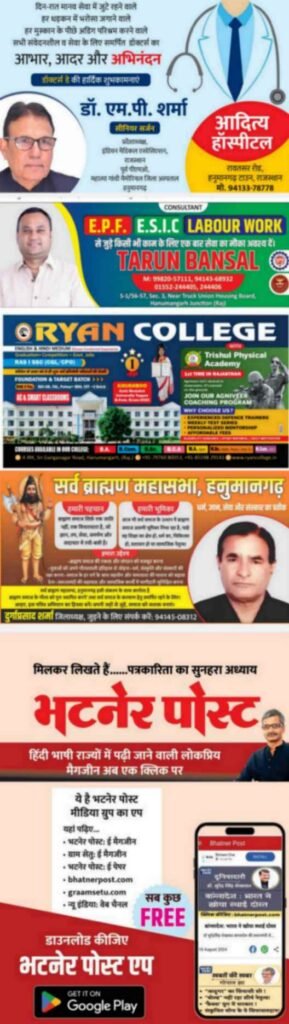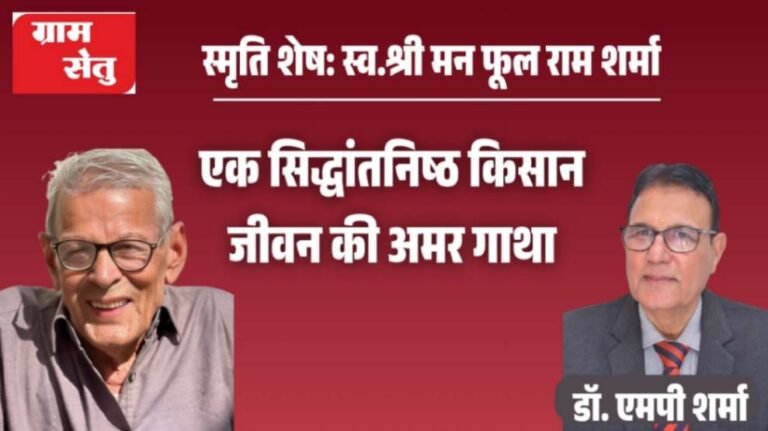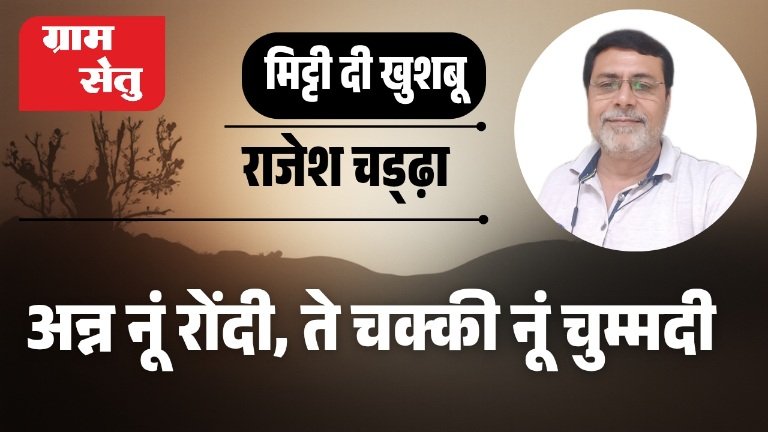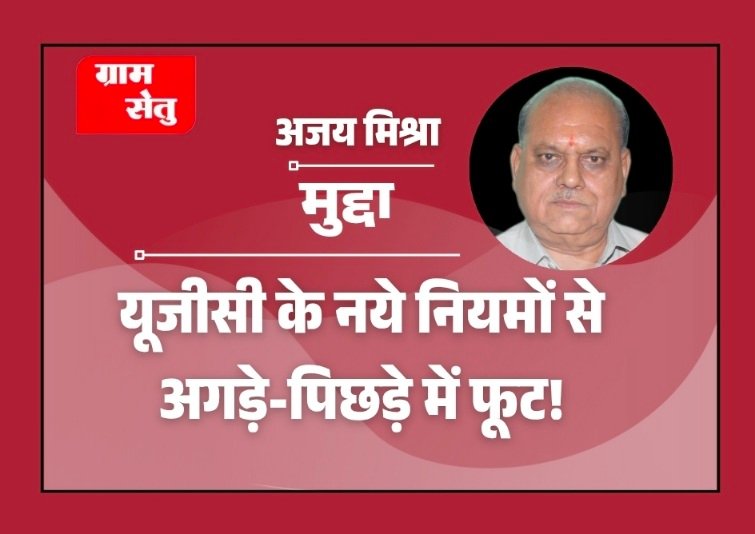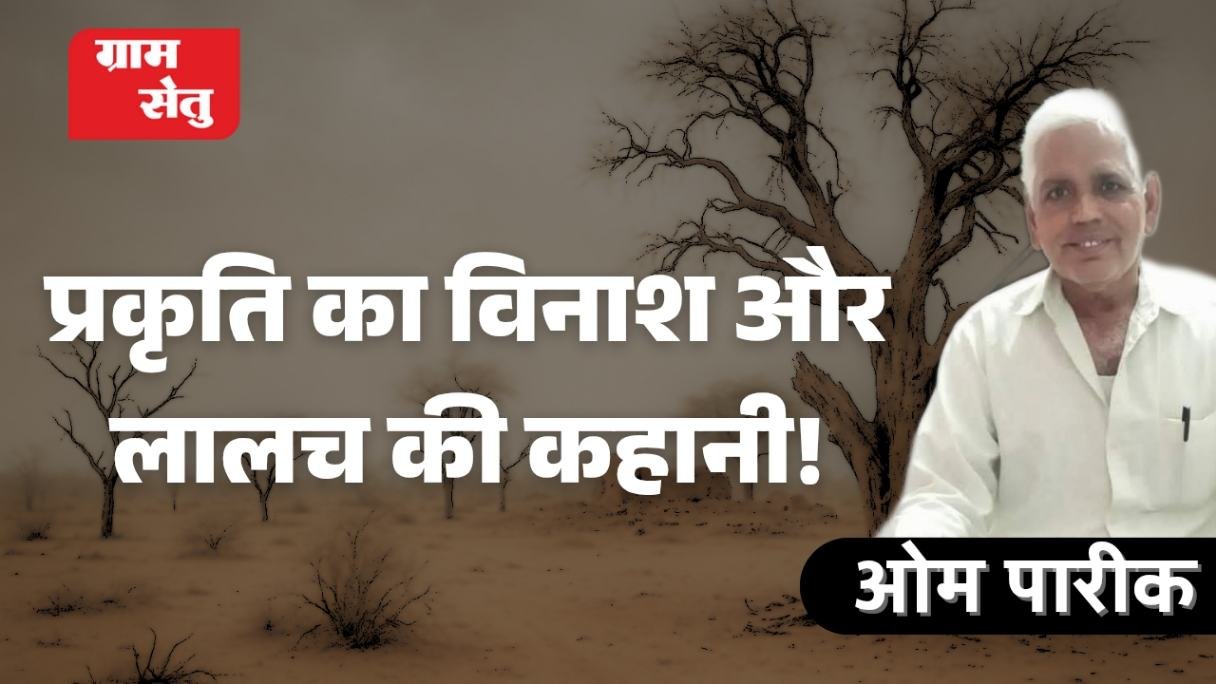
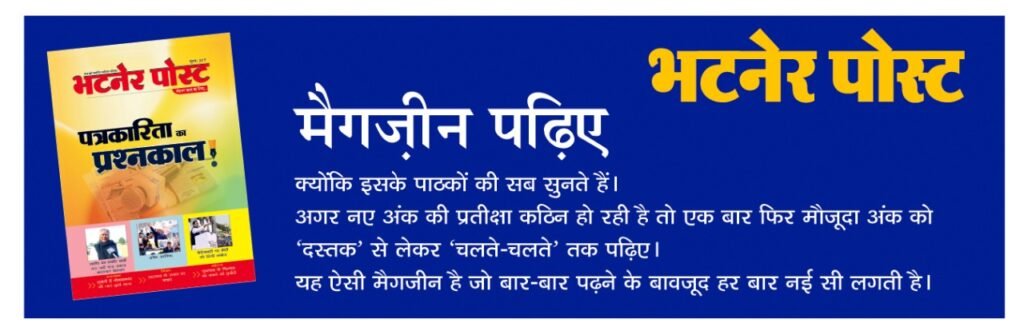
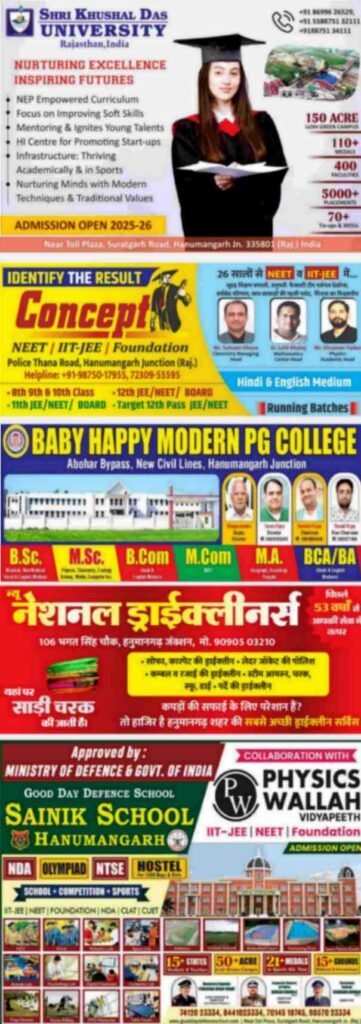
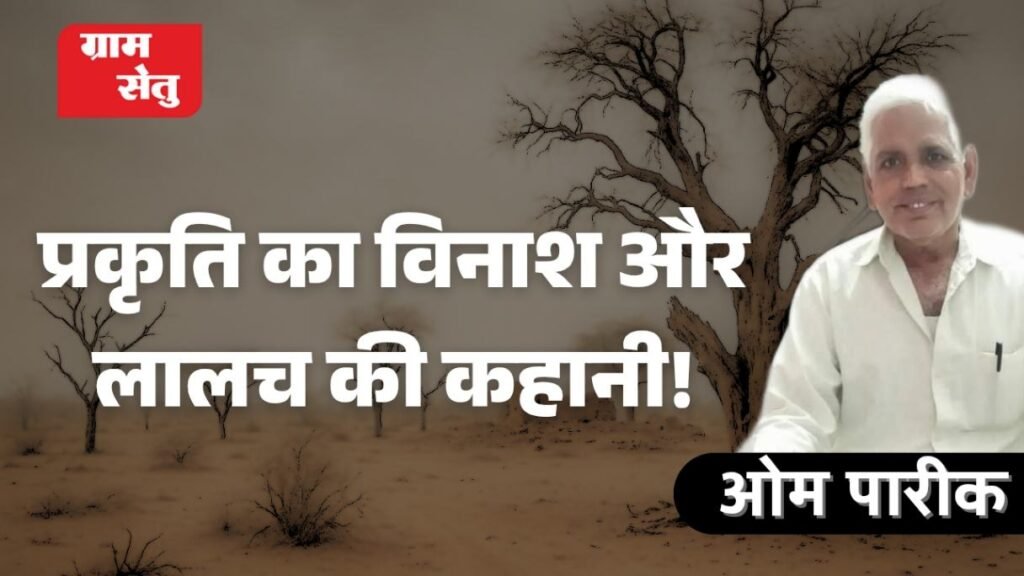
ओम पारीक.
मैं अक्सर पल्लू और उसके आसपास के ग्रामीण इलाकों में घूमता हूं। जब आज से आधी सदी पहले के दृश्य आंखों के सामने आते हैं और वर्तमान की सच्चाई से उनका मिलान करता हूं, तो एक गहरी टीस उठती है, क्या हमने अपने स्वार्थ के लिए प्रकृति की आत्मा को कुचल दिया है? वो धरती, जो कभी फोग, खेजड़ी, कांकेड़ा, बुई, केर, खींप, सेनिया और कुमठा जैसी वनस्पतियों से गुलज़ार रहती थी, अब अपनी जैव विविधता को खोज रही है। वह भूमि, जहां सैकड़ों साल पुराने जाल के वृक्ष सिर ऊँचा करके खड़े रहते थे, आज वहां वीरानी पसरी है। अब ये पेड़ दर्शन दुर्लभ हो गए हैं।

प्राकृतिक संसाधनों की दोहन प्रवृत्ति ने न केवल इन वनस्पतियों को मिटा दिया, बल्कि उस पूरे पारिस्थितिकी तंत्र को भी तहस-नहस कर दिया जो कभी मवेशियों, ऊंटों, हिरणों और नीलगायों का आधार हुआ करता था। मैं जब कभी गांव की पगडंडियों से गुजरता हूं तो वो दिन याद आते हैं, जब रेवड़, ऊंटों के टोले और गायों की बहुलता थी। अब ये केवल यादों में रह गए हैं।
मरु क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले इस इलाके में एक समय था जब भूमिगत जिप्सम का दोहन इस हद तक हुआ कि लोगों ने घर-आंगन तक से मिट्टी निकाल दी। जमीन को खेती योग्य बनाने के नाम पर औषधीय वनस्पतियों की बलि दे दी गई।
कभी यह भूमि बुई और कांकेड़ा जैसी औषधियों की खान थी। तुंबा, विश्लंबा और सेनिया जैसी वनस्पतियां अब खो चुकी हैं। यह बदलाव कोई स्वाभाविक परिवर्तन नहीं, बल्कि लालच की खेती का परिणाम है।

प्रकृति का दोहन केवल जंगलों तक सीमित नहीं रहा। कुएं, कुंड, जोहड़ और पायतन जैसे जल स्त्रोत, जो कभी ग्रामीण जीवन की धुरी हुआ करते थे, अब नवीन जल संसाधनों की चकाचौंध में उपेक्षित हो गए हैं। जंगलों की झाड़ियाँ और बेरी की बाड़बंदी, जो कभी चारा और फल का स्रोत थीं, अब नष्ट हो चुकी हैं। पहले हर गांव के बाहर बाड़े हुआ करते थे, प्राकृतिक रूप से बनी चारदीवारी, जो सामाजिक संरचना का हिस्सा थी। चुनावों में इन्हीं बाड़ों में गणना कर परिणाम तक घोषित होते थे। अब ना वो बाड़े हैं, ना वो परंपरा।
इस क्षेत्र में खेजड़ी और रोहिड़ा जैसे वृक्ष कभी अकाल और सूखे में भी जीवन की आशा बनकर खड़े रहते थे। लेकिन अब सदी पुराने ये दरख़्त दिखाई नहीं देते। रावतसर और पल्लू के पुराने मैदानों में जो जंगी खेजड़े होते थे, वे अब अतीत का हिस्सा बन चुके हैं। खेजड़ी केवल पेड़ नहीं था, वह एक परंपरा, एक जीवन शैली और स्थानीय पारिस्थितिकी का संरक्षक था। आज उसकी जड़ों को मनुष्य के लालच ने काट डाला।
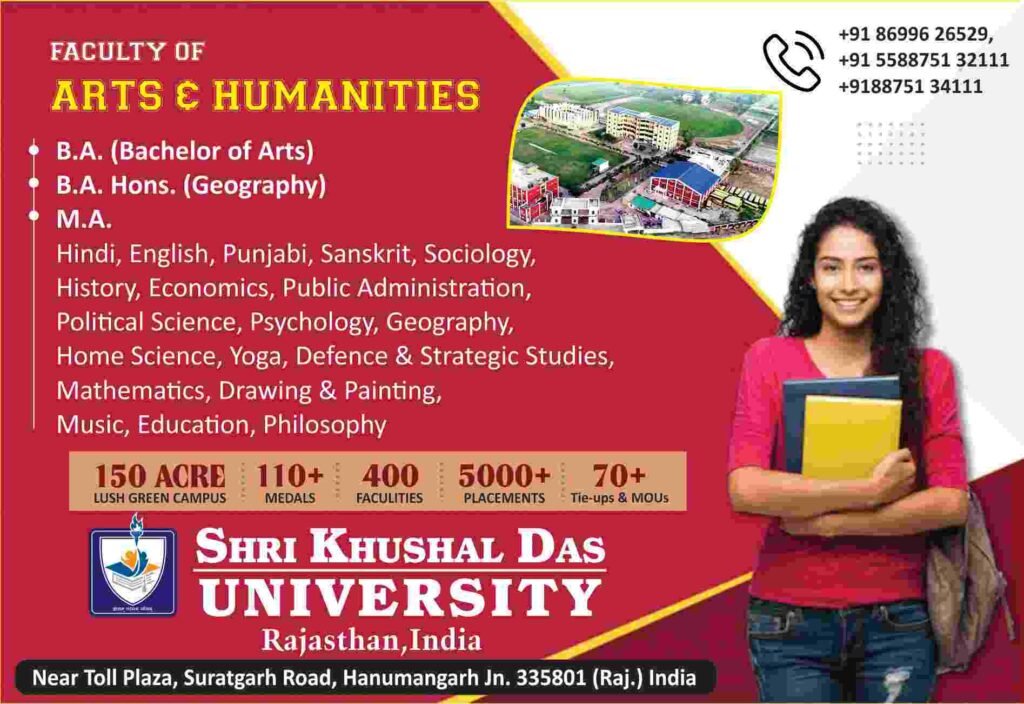
अब एक नया चलन शुरू हुआ है, कच्ची उपजाऊ मिट्टी को ज़मीन से निकाल कर ईंट भट्टों को बेचना। यह सिलसिला किसी बाहरी तत्व का नहीं, बल्कि स्वयं भू-स्वामी किसानों और भट्टा मालिकों की मिलीभगत का परिणाम है। बजरी, मुरम, क्ले मिट्टी का दोहन अब एक उद्योग बन चुका है। जो बालू रेत कभी बेकार समझी जाती थी, अब वो भी बिक रही है। मेरा देखा हुआ रतनगढ़ (चूरू जिला) की इकलौती पहाड़ी रणधीसर, अब केवल स्मृति शेष है, उसे पीसकर ग्रिट बना दिया गया। पुराने समय में उपयोग में लाया जाने वाला खारा चुना भी अब लुप्तप्राय हो गया है।
मूल वन्य जीव, सरीसृप और घास प्रजातियाँ अब यहां नहीं टिक पा रही हैं। खेती के लिए जंगलों को उजाड़ा गया, और बदले में जो मिला वो है एक खोखली हरियाली, जिसमें न तो चारा है, न जीवन। अब यहां के खेतों में केर, कांकेड़ा या झाड़ियों की उपस्थिति नहीं बची, जिन पर पशु निर्भर रहते थे। पशु, पक्षी और वन्य जीव अब धीरे-धीरे इस क्षेत्र को पलायन की स्थिति में छोड़ चुके हैं।
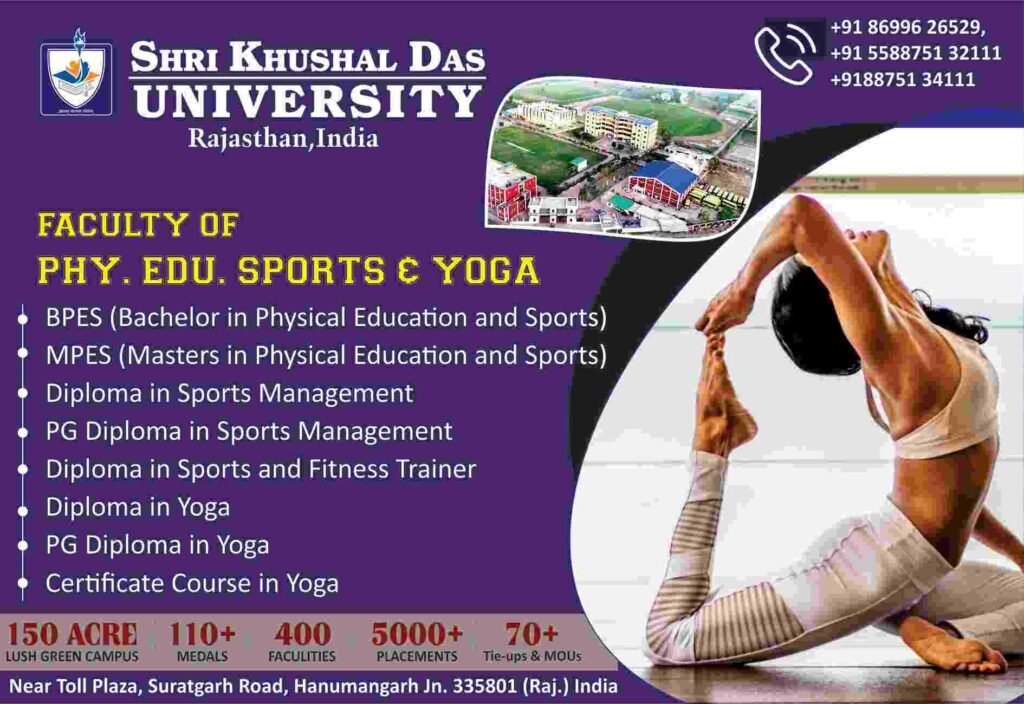
क्या हम सच में सभ्यता की ओर बढ़ रहे हैं? नहीं, बिलकुल नहीं। सभ्यताएं तभी टिकती हैं जब वे प्रकृति के साथ संतुलन बनाए रखें। लेकिन हमने अपने लाभ के लिए प्रकृति को जिस कदर रौंदा है, उसके परिणामस्वरूप अब हम एक ऐसी दुनिया की ओर बढ़ रहे हैं, जहां न हरियाली बचेगी, न संवेदनशीलता, और न ही सांस्कृतिक स्मृतियां।
अब भी वक्त है?हमें यह समझना होगा कि धरती बदला लेने में देर नहीं करती। यदि हमने प्रकृति को केवल एक संसाधन मानकर उसका दोहन जारी रखा, तो वो दिन दूर नहीं जब तापमान और जल संकट में हमारी तथाकथित सभ्यता दम तोड़ देगी।
(लेखक प्रकृति प्रेमी, वरिष्ठ पत्रकार और ग्रामीण परिवर्तन के साक्षी हैं)