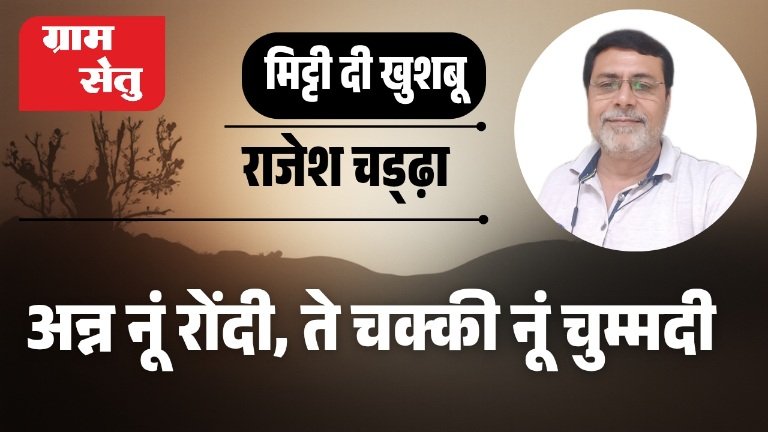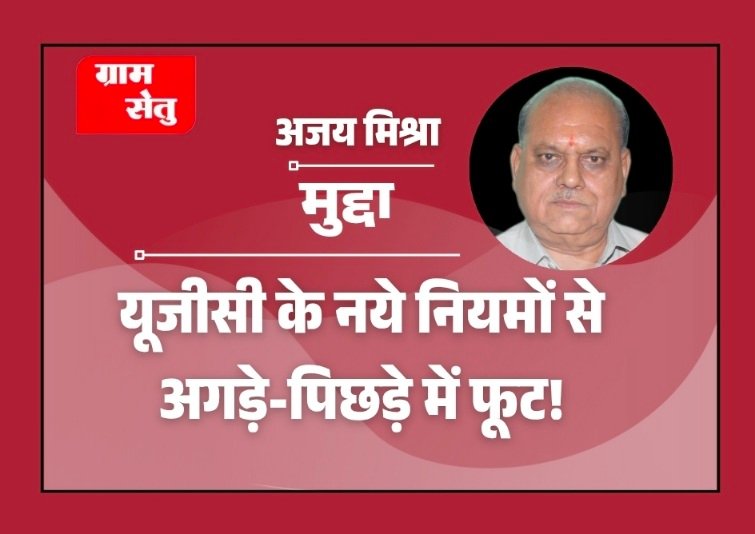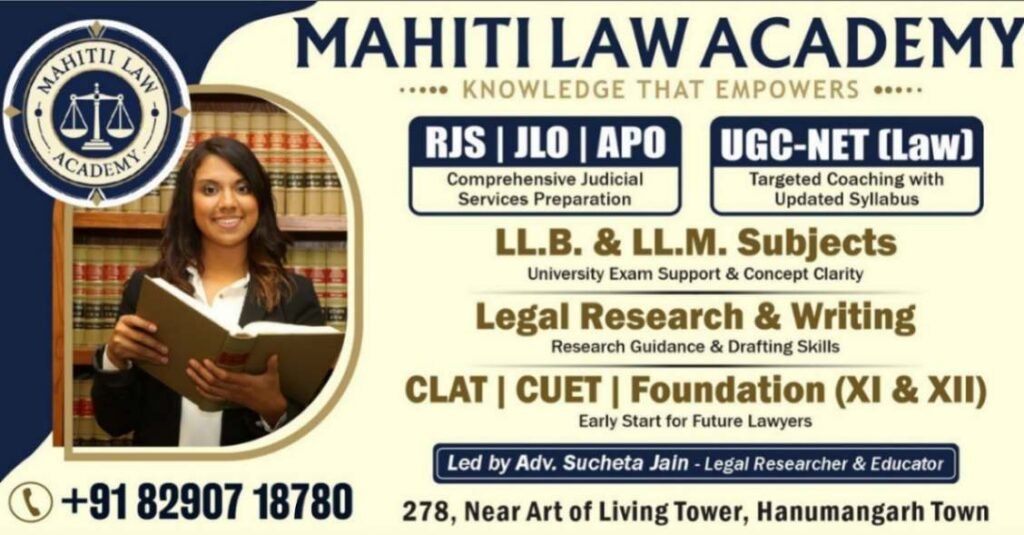



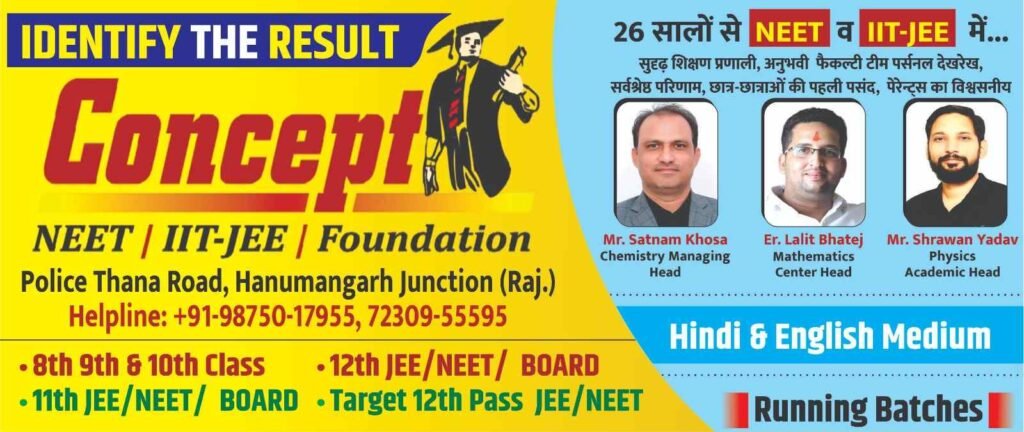

गोपाल झा.
बीकानेर को हम अक्सर भुजिया, रसगुल्ले और नमकीन की ‘राजधानी’ कहकर याद करते हैं। पर यह शहर केवल स्वाद का नहीं, बल्कि संस्कृति, परंपरा और जीवनदर्शन का भी संगम है। यहां की गली-कूचों में जब सूरज ढलता है, तो कोई और चीज़ सबसे पहले जीवन्त होती है, वह है पाटा। पाटा, जो महज़ लकड़ी या लोहे से बना तख्त नहीं, बल्कि मोहल्ले का साझा हृदय है; परिवार का पुरोधा, संस्कारों का पाठशाला और समय की स्मृतियों का अभिलेख भी।
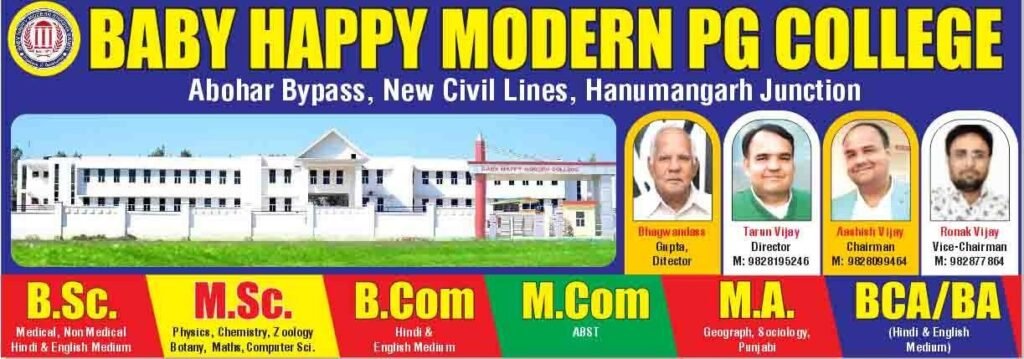
वरिष्ठ पत्रकार हरीश बी शर्मा ‘ग्राम सेतु डॉट कॉम’ से कहते हैं, ‘बीकानेर का पाटा एक जीवंत अख़बार की तरह है। यहां बैठकर लोग शहर-दुनिया की खबरें साझा करते हैं, दुख-सुख की समीक्षा करते हैं और समाज के साथ बने रहने का अभ्यास करते हैं। सचमुच, पाटा सिर्फ़ बैठक नहीं, बल्कि संवाद का सेतु है।’ किसी भी परिवार में जब मांगलिक अवसर आता है, तो सजी-धजी महिलाएं मंगलगीतों की लहरियां इन्हीं पाटों पर बैठकर बिखेरती हैं। वहीं, गमी के समय यही पाटे सांत्वना देने वाले पड़ोसियों के गवाह बनते हैं। पाटा जीवन की हर ऋतु में सहभागी है, खुशी हो या गम। यही कारण है कि बीकानेर में पाटा परिवार और समाज के मुखिया की तरह माना जाता है।
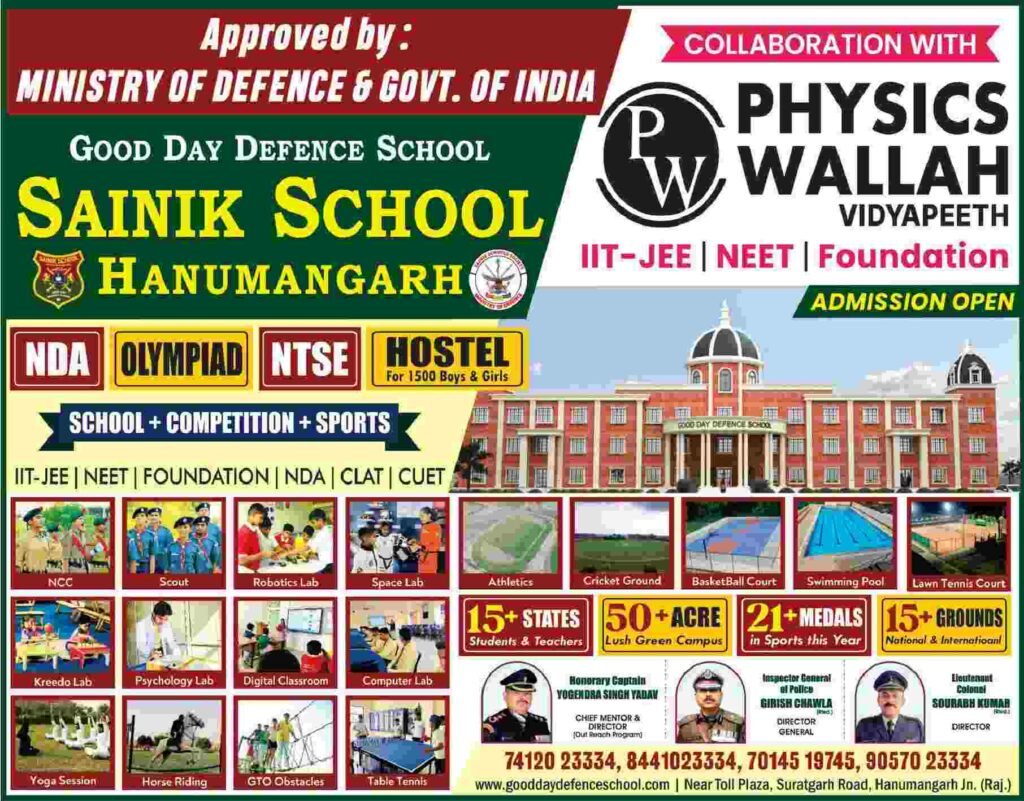
आमतौर पर पाटे चार पग के होते हैं, लेकिन बीकानेर में छह और सात पग वाले पाटे भी मिलते हैं। कुछ पाटे शताब्दी से भी पुराने हैं, जिन पर समय की छाप कलात्मक नक्काशी के रूप में दर्ज है। शहर में 1950 से पहले तक 120 पाटे थे, जिनमें से अधिकांश लकड़ी के बने थे। आज भी 110 पाटे जीवित परंपरा की तरह खड़े हैं, हालांकि कई जीर्ण-शीर्ण अवस्था में हैं।

‘पाटा परम्परा एवं परिवर्तन’ के लेखक डॉ. राजेन्द्र जोशी लिखते हैं कि बीकानेर में पाटों का इतिहास तीन शताब्दियों से भी पुराना है। परकोटे वाले इस शहर में 17वीं सदी से पाटे लोकजीवन का हिस्सा बने। जबकि लोक मान्यता के अनुसार पाटा संस्कृति की जड़ें 500 वर्षों तक पीछे जाती हैं।
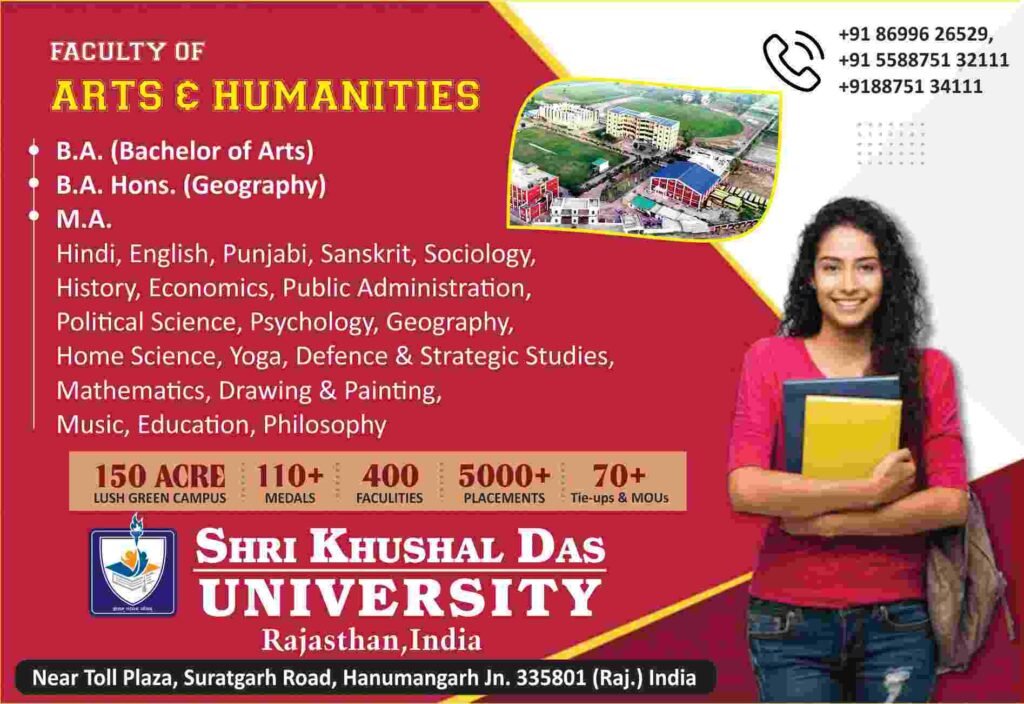
वास्तुविद आरके सुतार के अनुसार, ‘पाटा दरअसल शहरी वास्तु का अनूठा अंग है। यह केवल चौपाल नहीं, बल्कि उस समय के नगर नियोजन का हिस्सा है, जहां सामुदायिक जीवन को टिकाऊ आधार मिला।’ परिवार में पाटा को ‘तख्त’, ‘बाजौट’ या ‘चौकी’ कहा जाता है, जबकि मोहल्लों में इसे ‘बैठक’ या ‘चौक’ भी कहते हैं। किंतु ‘पाटा’ शब्द ही लोकजीवन में सबसे ज्यादा प्रचलित हुआ। यही कारण है कि बीकानेर को लोग पाटा गजट, पाटाबाजी और पाटा संस्कृति जैसे नामों से भी पहचानने लगे।
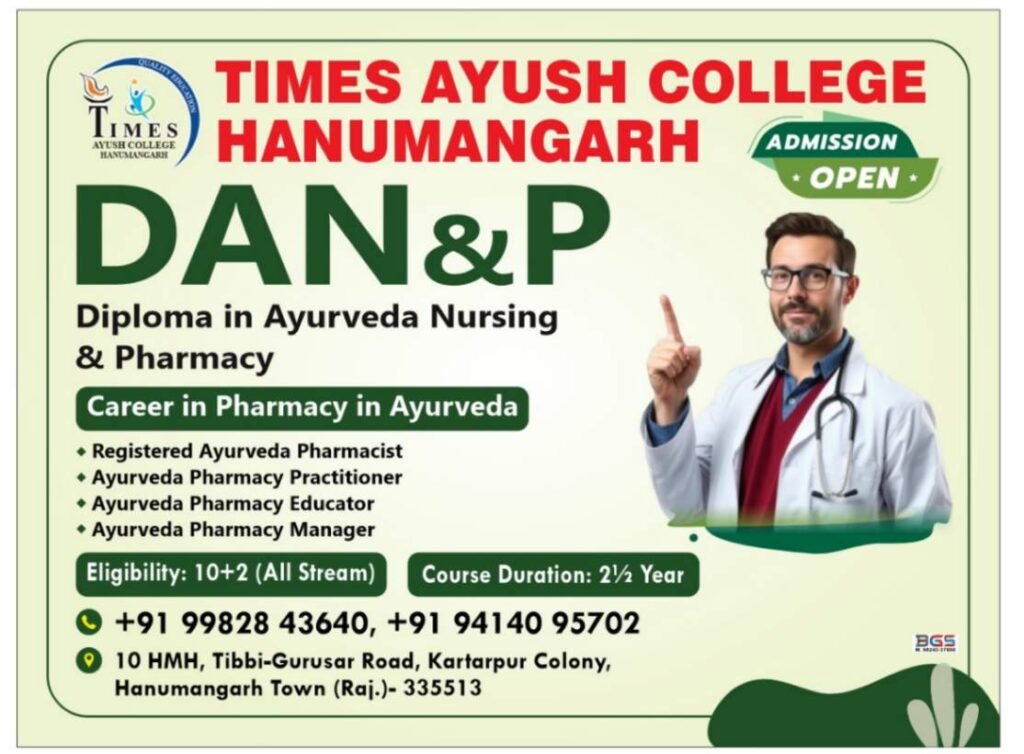
भजन-कीर्तन, रम्मतें, नृसिंह चतुर्दशी का मेला, होली की चौपालें, सबका केंद्र पाटा है। यही नहीं, ताश-शतरंज, चौपड़ के खेल से लेकर देश-विदेश की राजनीतिक चर्चाएं भी इन्हीं पाटों पर होती हैं। शाम ढलते ही पाटों पर रौनक बढ़ती है और देर रात तक चर्चा, हंसी और विचारों की गूंज बनी रहती है।
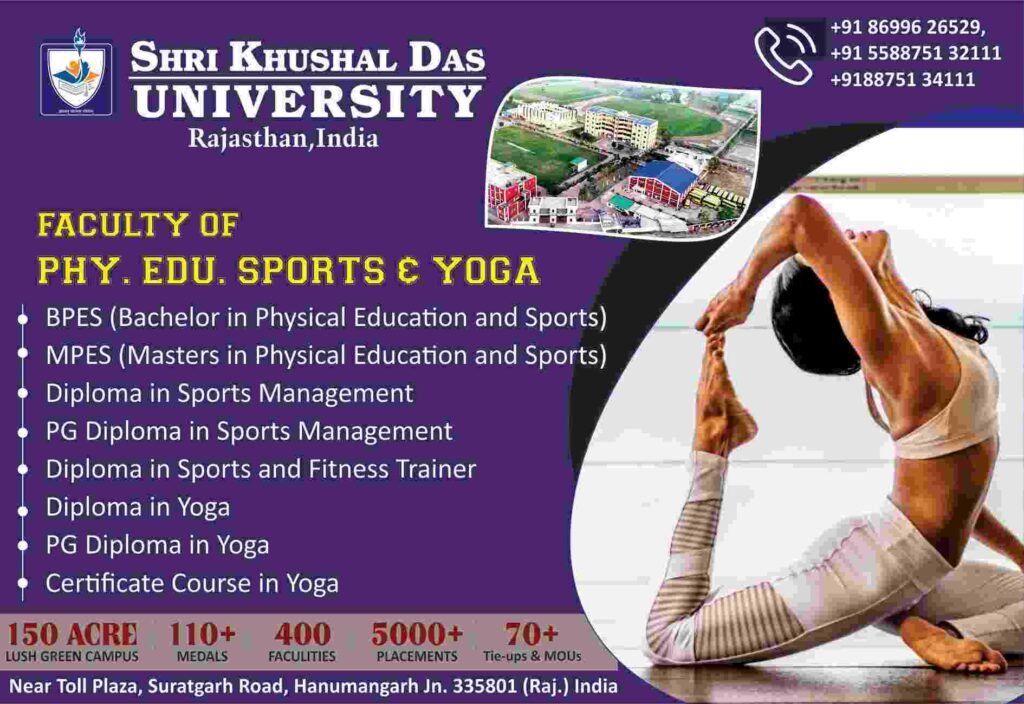
वरिष्ठ पत्रकार हरीश बी शर्मा का कहना है, ‘आज के डिजिटल युग में जब लोग स्क्रीन से चिपककर अलग-थलग हो रहे हैं, पाटा हमें संवाद की जीवंतता की याद दिलाता है। यह मोहल्ले को परिवार बनाता है।’ बीकानेर का पाटा केवल हिंदुओं का नहीं, बल्कि मुसलमानों का भी उतना ही है। यही पाटा सांप्रदायिक सौहार्द का सबसे बड़ा प्रतीक है। गुवाड़ों और चौकों में बैठकर दोनों समुदाय एक-दूसरे के जीवन में साझेदारी करते हैं। यही वह संस्कार है जिसने बीकानेर की पहचान को गढ़ा है।

संस्कृति प्रेमी मनोज मोदी कहते हैं, जब मोहल्ले का पाटा सजता है तो वह केवल लकड़ी या लोहे का तख्त नहीं रहता, वह जीवन का उत्सव बन जाता है।’ आज भी बीकानेर के 110 पाटे शहर की आत्मा की तरह खड़े हैं। कुछ नये सिरे से संवार दिए गए हैं, कुछ मरम्मत की प्रतीक्षा में हैं। पर उनकी उपयोगिता और प्रासंगिकता जस की तस है। सवाल यही है कि क्या हम आने वाली पीढ़ियों को इस परंपरा से जोड़ पाएंगे?
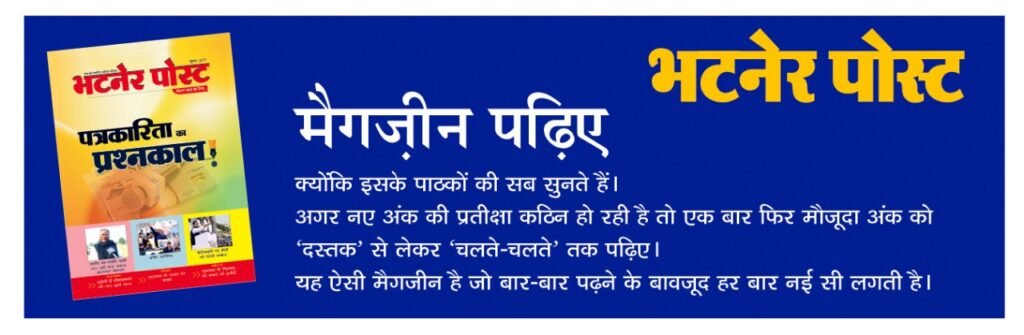
वास्तुविद आरके सुतार का सुझाव है कि नगर निगम और सांस्कृतिक संस्थाओं को मिलकर पाटों को सिटी हेरिटेज प्रोजेक्ट के रूप में संरक्षित करना चाहिए। इससे न केवल परंपरा जीवित रहेगी बल्कि पर्यटन को भी नया आयाम मिलेगा।
बीकानेर का पाटा सिर्फ़ चौपाल नहीं, यह संस्कृति का जीवंत ग्रंथ है। इसमें समय, समाज और संवेदना के असंख्य अध्याय दर्ज हैं। यहां बैठना मानो उस जीवन को जीना है, जो साझा है, सहिष्णु है और संस्कारों से भरा हुआ है। यह पाटा ही है जिसने बीकानेर को केवल स्वाद नहीं, बल्कि संवाद और संस्कृति का शहर बनाया है।