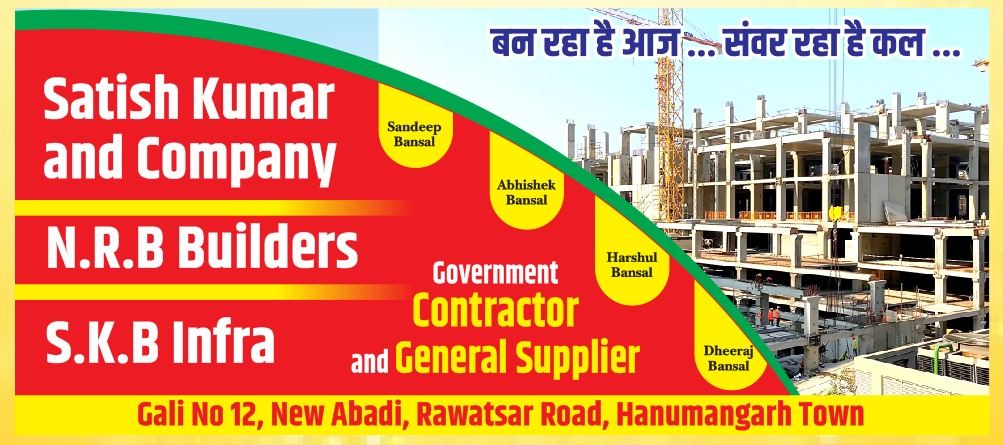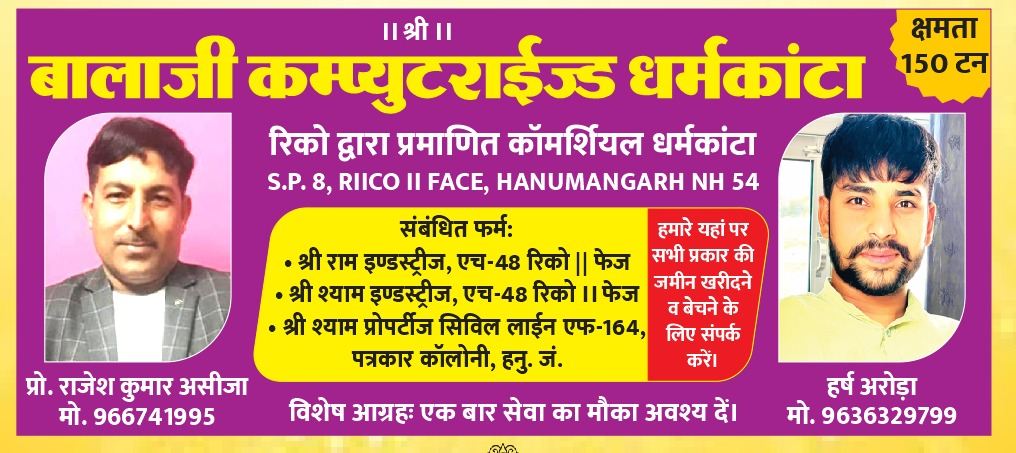आर्किटेक्ट ओम बिश्नोई.
अक्टूबर का महीना अपने यौवन की तरफ बढ रहा था। वो अपनी ढाणीं में बैठा धूप सेक रहा था, चारपाई पर जो थार के ऊंचे टीले पर बनीं थी। उसके मोबाइल पर विडियोकॉल बज उठी। उसने कॉल उठाई तो प्रोफेसर बोल उठीं। ‘तुम हर बार की तरह इन दिनों फिर फुर्र हो गए। शहर की कंक्रीट छोडकर रेत की तरफ?’
सुनते ही उसके चेहरे पर मुस्कुराहट पसर गई। बोला-‘मैं इन दिनों सुबह थार की जुल्फों की लटों को करीने से सजाती हवाओं के किस्से देखता हूं। ढाणी के इर्द-गिर्द पसरी भोर की ठंडी रेत को निहारत हुए।’ इतना सुनते ही प्रोफेसर भी खिलखिला उठीं। बोलीं-‘इस बात पर तुम कभी सीधे क्यों नहीं कहते चीजों को ?’
वह बोला-‘सीधा-सीधा ही तो बता रहा हूं। मतीरे मीठे होने लगते इन दिनों। धीमे-धीमे बहती हवा थार से जो रेत की झुल्फों को सुलझाती है प्रेम से इन दिनों।

हां सुनों प्रोफेसर! ये राज मुझे मेरे दादा ने बताया था। रेत का हवा का और मतीरों, काचर के पक जाने का। वो कहते थे कि बेटा आसोज कार्तिक का महीना आते-आते हवायें जेठ के महीने की तेजी छोडकर धीमे हो जाती हैं और थार की रेत की जुल्फों को सुलझाती है बहुत प्यार से। इन्हीं दिनों काचर पकने लगते हैं, मतीरे मीठे होने लगते हैं खेतों में और किरसे के खेतों से दीयाली वाले दिये जलते हैं। वो कहते थे कि जहां भी रहना, लौटते रहना। इन महीनों में ढाणी की ओर। खेतों की ओर, रेत की ओर। फिर मेरा तो जन्मदिन भी इन मतीरे मीठे होने वाले महीनों का है तो लौट आता हूं गांव। रेत की सुलझी लटें देखने, जिन्हें इन दिनों हवाओं ने अपनी अंगुलियों से सहलाकर सुलझाई हैं।’
‘वाह क्या प्रेम है तुम्हारा रेत हवाओ से।’ प्रोफेसर बोल उठीं।

वह हंसा और बोला-‘हां, है तो थोडा इसे पी लूं। जी लूं, भर लूं भीतर फिर शहर आना ही आना है लौटकर। अरे हां, सुनो प्रोफेसर! तुम साहित्य लिखती हो। बांचती हो मंचों पर और जानती भी हो, इश्क, प्रेम कभी बुढा होता। भला भोर की किरण की तरह चमक उठता फर्श से अर्श तलक। तो कुछ रेत हवा की जुगलबंदी की संगत। कुछ मित्रो की संगत में मैं भी सीख ही गया और लगा रहता हूं लकीरों को सुलझाने में आर्किटेक्चर करते-करते। इन दिनों जब रेत मतीरे मीठे कर रही है और धूप भोर की सुहानी होने लगी है। सुहानी भोर की हवायें मेरी लकीरों को भी रौशन करे। प्रोफ़ेसर! मैं भी चाहता हूं अपनी खींचीं लकीरों से बने घरों में धूप किसी खिडकी से इन दिनों भोर में उतरे बैडरूम, लिविंग रूम, बरामदे में और सहला दे माही को, हीर को, घर को बच्चों को और गुजर जाए अपनी राह। प्रोफेसर मुझे तो धूप, हवाओं, रेत, आकाश, पौधों की संगत ने ही तो बहुत कुछ सिखाया है किताबों के बाद। ये मरजाणीं सर्द महीनों की भोर की धूप तो मुझ से कहती है, सुनो आर्किटेक्ट! प्रेम भी कभी बंधता भला वो तो स्पार्क करता रहता है। कभी फर्श पर, कभी चेहरों पर, कभी मुंडेर पर।’
प्रोफेसर ने कहा-‘देखो, मित्रो की संगत तुम में गहरे उतर बोलने लगी है। जब लौट आओ खबर करनां कॉफी भोर में बरामदे में होगी। भोर की धूप की संगत में सिप करेगें।’