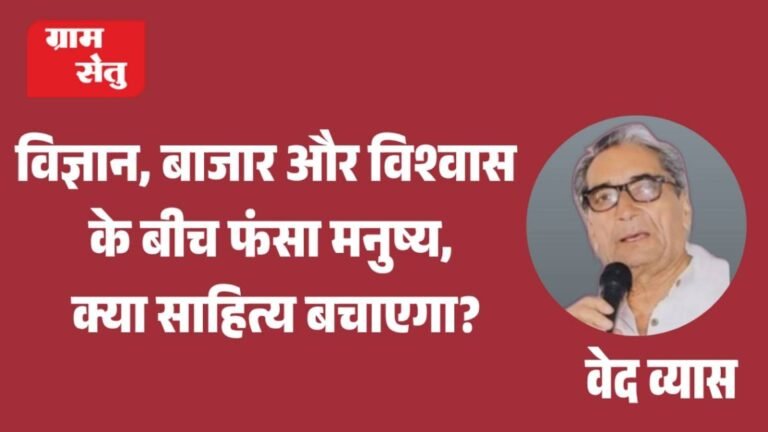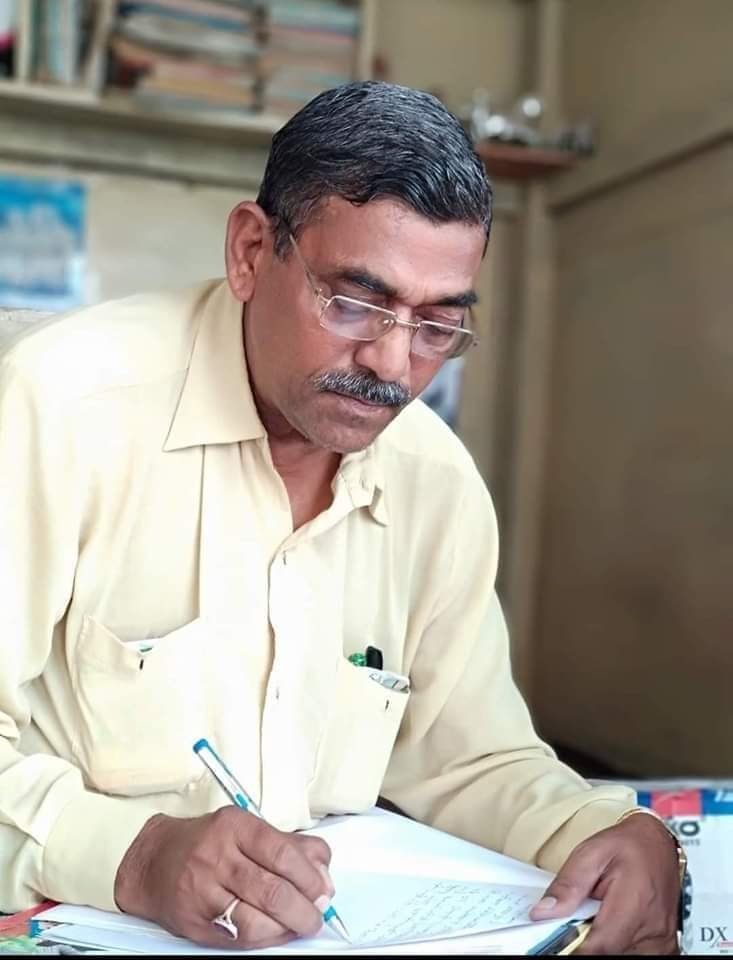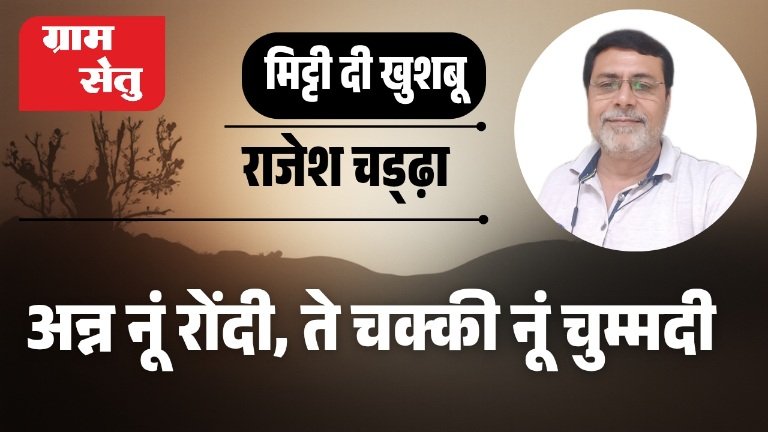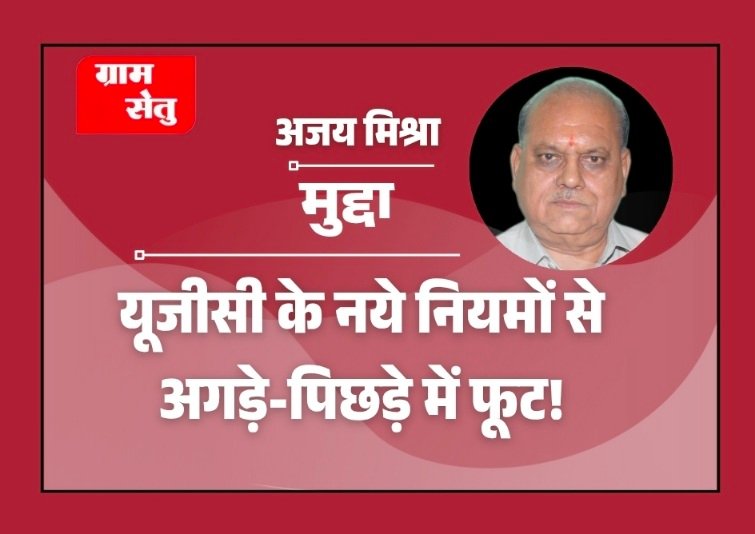गोपाल झा.
करीब पांच साल पुरानी बात है। एक सेमीनार में मुझे आमंत्रित किया गया था। आमंत्रण तो औपचारिक भाषण देने का था, मगर मैं उन लोगों में से हूं जो मंच से बोलने से ज्यादा सामने बैठे चेहरों की आंखों में पढ़ने में रुचि रखते हैं। मैंने माइक संभाला और युवाओं के साथ संवाद शुरू कर दिया। सच पूछिए तो युवाओं से बात करने का हमेशा अपना एक अलग ही सुख होता है। वे किसी बने-बनाए फ्रेम में नहीं सोचते, बल्कि उनके विचारों में ऊर्जा होती है, उलझन होती है, और अकसर सत्य को छूने की एक तीव्र लालसा भी। लेकिन उस दिन जो महसूस किया, वह कुछ अलग था। छात्रों की बातचीत, उनकी शंकाएं, उनके तर्क, सब किसी न किसी रूप में ‘जाति’, ‘धर्म’, ‘क्षेत्र’ और ‘पहचान’ के घेरे में सिमटे हुए थे। हर सवाल के पीछे जैसे कोई अदृश्य दीवार थी, जो उन्हें एक व्यापक दृष्टिकोण से वंचित कर रही थी।
मुझे निजी तौर पर झटका-सा लगा। क्या हमारी शिक्षा व्यवस्था युवाओं को आज भी इन सीमाओं से ऊपर उठने की प्रेरणा नहीं दे पा रही? क्या हमारा समाज अब भी संकीर्ण पहचान की रेखाओं में अपने भविष्य को बाँधने पर आमादा है? मैंने उनसे पूछा, ‘आप में से कौन अपने आपको केवल एक धर्म, जाति या क्षेत्र का प्रतिनिधि मानता है?’ काफी हाथ उठे। फिर पूछा, ‘और कौन खुद को सिर्फ ‘छात्र’ या ‘नागरिक’ या ‘मानव’ के रूप में देखता है?’ इस बार हाथ कम थे, मगर जो थे, वे आशा की किरण जैसे लगे।

मैंने तब उन्हें एक उदाहरण दिया, ‘मान लीजिए मैं खुद को केवल एक ब्राह्मण, केवल एक हिंदू, या केवल राजस्थान से आने वाला व्यक्ति मानता, तो मेरी दुनिया कितनी सीमित होती! लेकिन मैं पत्रकार हूं। पत्रकारिता मेरी ‘बिरादरी’ है, एक ऐसा वर्ग जो हर जाति, धर्म, भाषा और क्षेत्र के लोगों को समेटे हुए है। जब मैं अपनी बिरादरी के लोगों के साथ घुलता-मिलता हूं, तो मैं पंजाब की मिठास, बंगाल की कविता, केरल की सोच और असम की धरती को महसूस कर पाता हूं। मैं मुसलमान साथियों की इबादत में डूबता हूं, ईसाई मित्रों के क्रिसमस में रोशनी देखता हूं, सिखों की सेवा-भावना को सीखता हूं और आदिवासी लोककथाओं में गुम हो जाता हूं। यह पत्रकारिता की बिरादरी मुझे ‘वर्ग’ में लेकर आई है, एक ऐसा वर्ग जो समावेशी है, जो सीमाओं से ऊपर है।’ संतोष की बात, कुछ छात्र गंभीर हो गए, कुछ की आंखों में सवाल तैरने लगे। मगर संवाद का बीज बो दिया गया था।
विविधता का यह अनुभव मेरे लिए कोई नवाचार नहीं था, यह तो मेरे जीवन का हिस्सा रहा है। पत्रकार के रूप में जब मैं किसी समारोह को कवर करता, किसी आंदोलन की रिपोर्टिंग करता या किसी गांव की सच्चाई सामने लाता, तो वहां केवल घटनाएं नहीं होती थीं, वहां संस्कृति होती थी, संवेदना होती थी, और होती थी इंसानी जिजीविषा की विविध परतें।
सच पूछिए तो विविधता केवल अंतर नहीं है, वह ‘आमंत्रण’ है, एक ऐसा न्यौता जो हमें किसी और की दुनिया में प्रवेश करने की अनुमति देता है।
रमजान के दौरान रोज़ा खोलने के समय जब मुस्लिम दोस्तों के साथ बैठता हूं तो उस सूखी खजूर और पानी के घूंट में महसूस किया गया अपनत्व किसी भी दावत से बड़ा होता है। वहीं मुझे समझ आया कि ‘धर्म’ अलग हो सकते हैं, पर भावनाएं नहीं।
आज जब 21 मई को हम विश्व सांस्कृतिक विविधता दिवस के रूप में मनाते हैं, तो यह केवल एक प्रतीक नहीं, बल्कि एक आह्वान है, हम अपने संकीर्ण दायरे से बाहर निकलें, और उस विराट मानवता से जुड़ें जो हमारे ही आस-पास सांस ले रही है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि सांस्कृतिक विविधता कोई खतरा नहीं, वह तो जीवन का उत्सव है।
विविधता से घबराने की नहीं, उसे अपनाने की जरूरत है। जैसे संगीत में विविध राग मिलकर एक संपूर्ण रचना बनाते हैं, वैसे ही अलग-अलग संस्कृतियां मिलकर इस संसार को सुंदर बनाती हैं। जिस दिन हम केवल अपनी जाति या धर्म तक सीमित रह जाते हैं, उस दिन हम अपने अनुभवों की दुनिया को सिकोड़ देते हैं। लेकिन जब हम अपने विचारों में विविधता को जगह देते हैं, तो हम पूरी दुनिया को जीने लगते हैं।
वह कॉलेज का कार्यक्रम मेरे लिए भी एक सीख था। संवाद के अंत में कई छात्रों ने कहा, ‘सर, अब समझ में आया कि केवल अपने धर्म या जाति से जुड़ना हमें कितना सीमित कर देता है।’ यह सुनकर मन में संतोष हुआ, शायद कोई दिशा मिली होगी।
आज जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं, तो वह अनुभव एक दीपक की तरह लगता है, जो न केवल दूसरों के लिए, बल्कि मेरे अपने लिए भी मार्गदर्शक बन गया। इसीलिए मैं बार-बार यही कहता हूं, ‘कट्टर बने रहने से बेहतर है, उदार बनो। अपनी पहचान पर गर्व करो, लेकिन दूसरों की पहचान का सम्मान भी करो। हर संस्कृति में कुछ नया है, कुछ सिखाने वाला है, और यही विविधता, यही रंग-बिरंगी मानवता, इस जीवन को अनमोल बनाती है।’