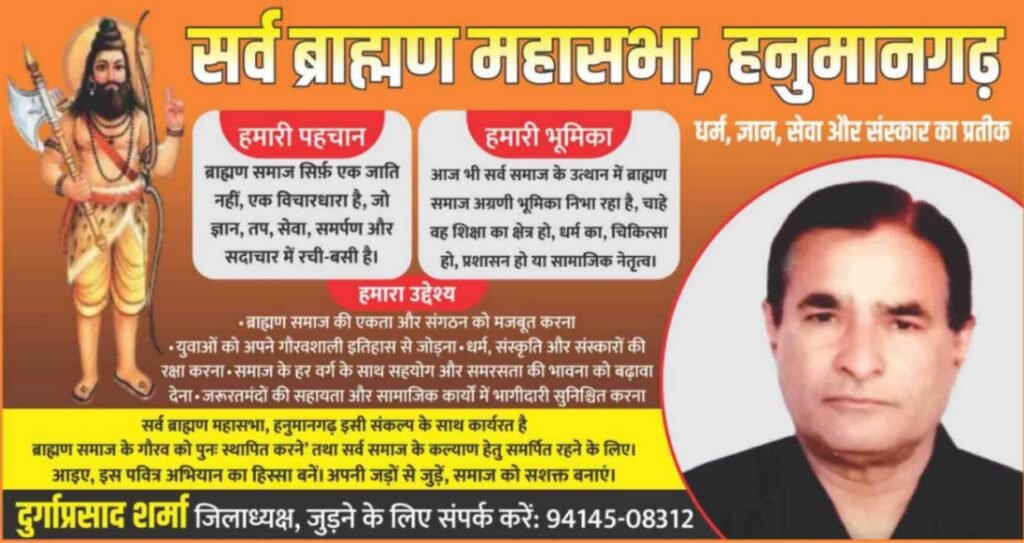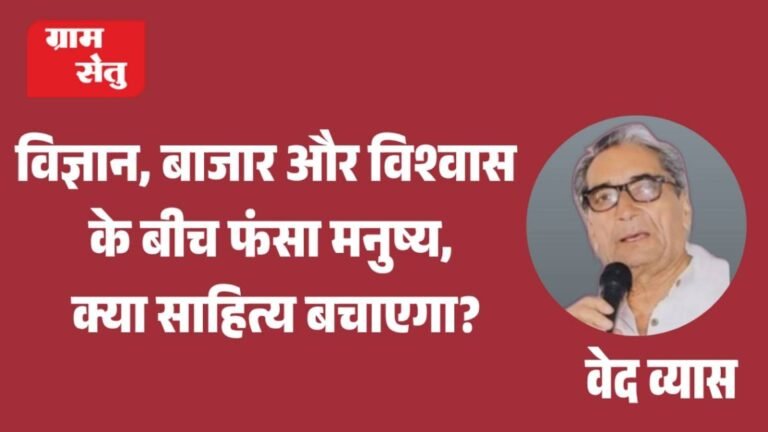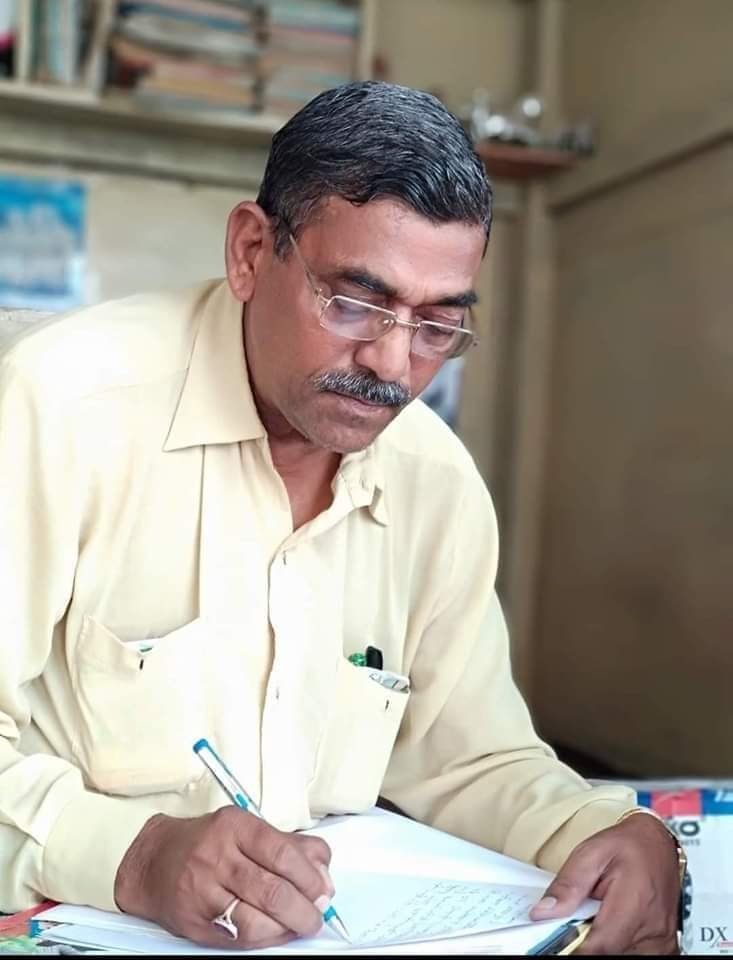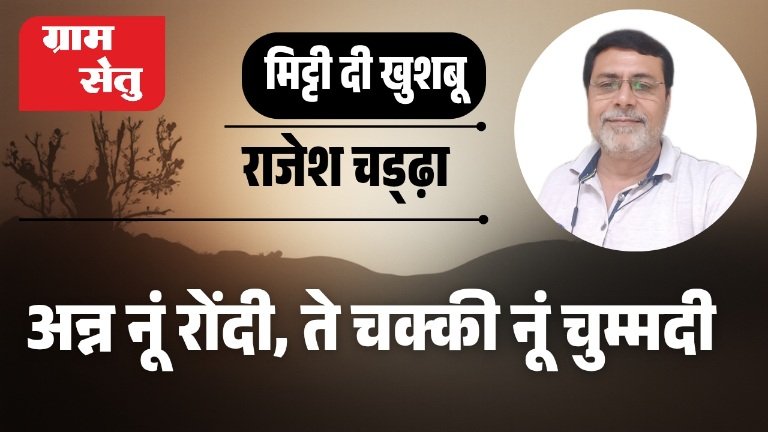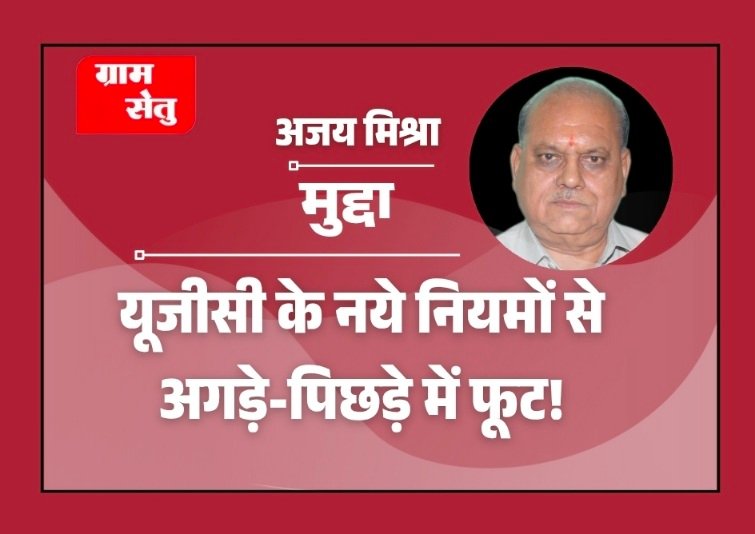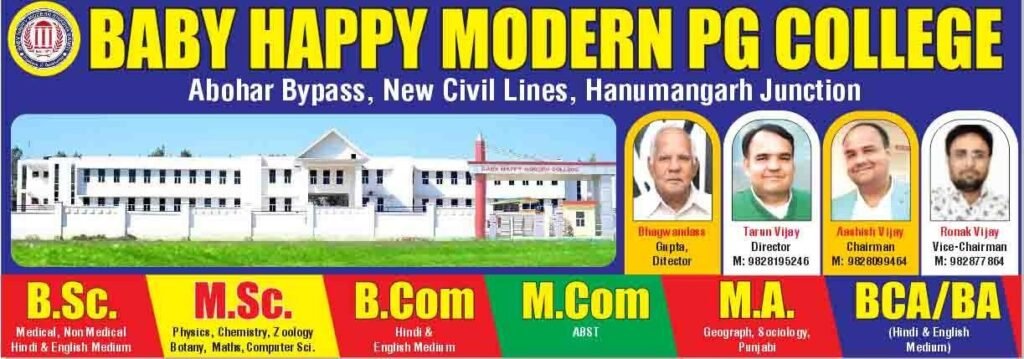


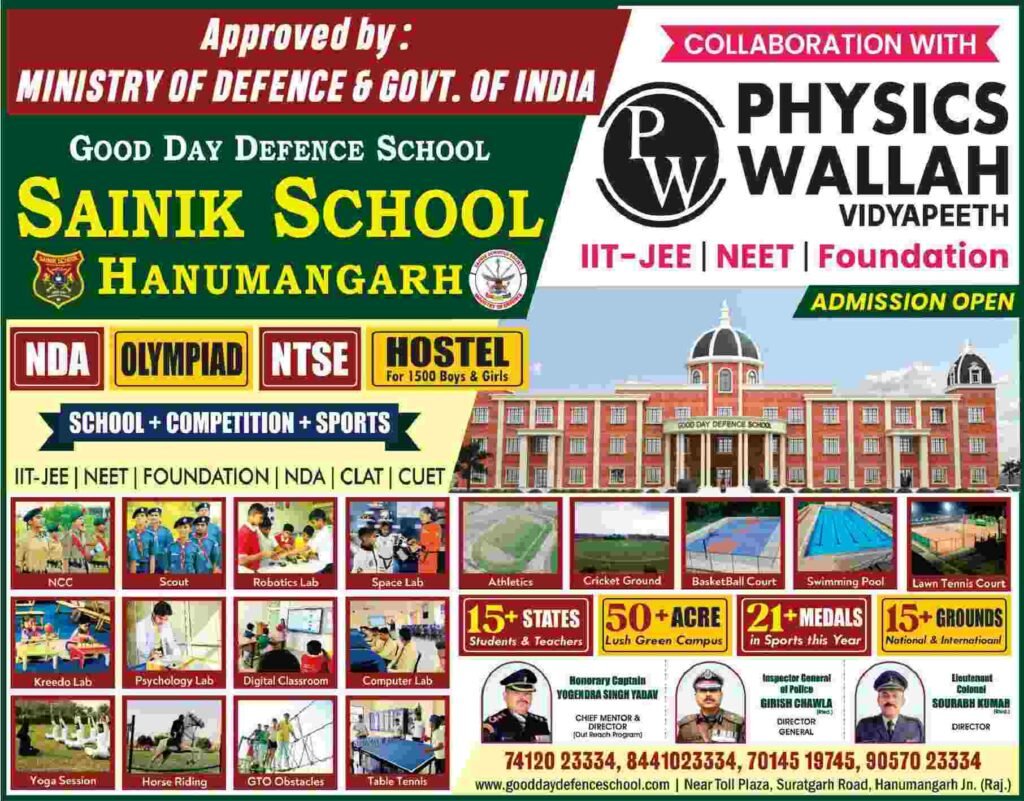
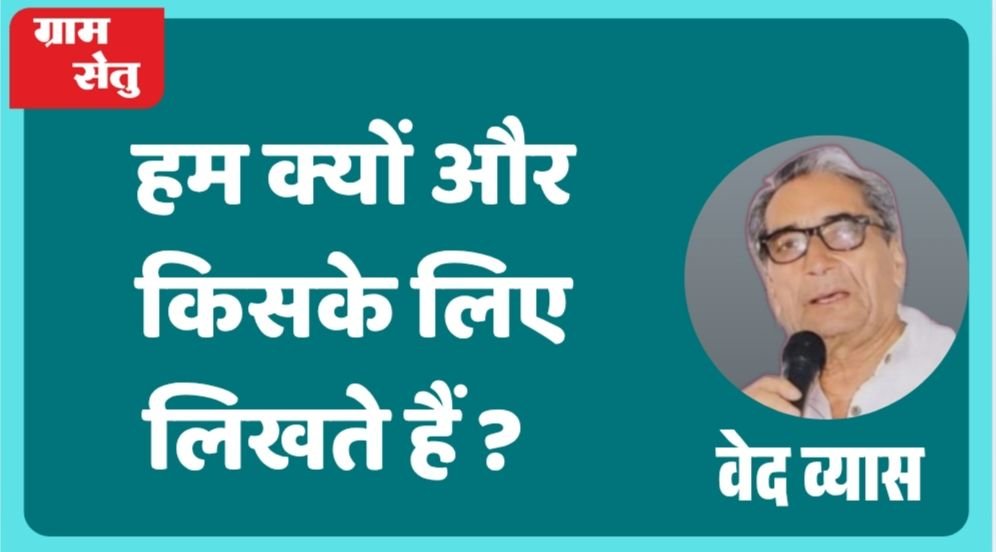
वेदव्यास.
मनुष्य, प्रकृति और शब्द की चौरासी यात्राएं पूरी करने के बाद मुझे लगता है कि साहित्य ही समाज व समय की चेतना का मूल स्वर है जो हजारों साल से मनुष्य के शब्द, दिशा और संभावना तय कर रहा है। आज भी लेखक और पाठक के बीच शब्द ही विचार और व्यवहार को तय करता है। संत तुकाराम ने इसी शब्द और साहित्य के लिए कहा था कि-’शब्द ही/एकमात्र रत्न है/जो मेरे पास है/शब्द ही/एकमात्र वस्त्र है/ जिन्हें मैं पहनता हूं/शब्द ही/एकमात्र आहार है/जो मुझे जीवित रखता है/शब्द ही/एकमात्र धन है/जिसे मैं लोगों में बांटता हूं।’
शब्द और समय की यह अंतर्यात्रा हमें बताती है कि संसार के सभी मनुष्य चाहे वह किसी भी जाति, धर्म, राष्ट्र अथवा भाषा के हों उनके अधिकार समान है और उन सबका एक ही लोकमंगल का उद्देश्य है। क्रांतिकारी भगतसिंह इसीलिए कहते हैं कि-हमें यह बात सदैव ध्यान में रखनी चाहिए कि हम सब मनुष्य ही यत्र-तत्र सर्वत्र सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं राजनैतिक समानता के लिए ही संघर्ष कर रहे है। क्योंकि समानता और विकास ही न्याय के दो पहलू हैं। हजारों साल की मानव संस्कृति को नई परिभाषा देते हुए ही कथाकार प्रेमचंद ने 9 अप्रैल 1936 को भारत के पहले लेखक संगठन (प्रगतिशील लेखक संघ) के उद्घाटन उद्बोधन में कहा था कि-’साहित्यकार का लक्ष्य केवल महफिल सजाना और मनोरंजन का सामान जुटाना नहीं है, उनका दरजा इतना न गिराइए। वह देशभक्ति और राजनीति के पीछे चलने वाली सच्चाई भी नहीं, बल्कि उनके आगे मशाल दिखाती हुई चलने वाली सच्चाई है।’ अतः अगर तुझे जीवन के रहस्य की खोज है तो वह तुझे संघर्ष के अलावा और कहीं नहीं मिलने का। सागर में जाकर विश्राम करना नदी के लिए लज्जा की बात है। आनंद के लिए मैं (लेखक) घोंसले में भी बैठता नहीं। कभी फूलों की टहनियों पर तो कभी नदी के तट पर होता हूं। सदियों से चली आ रही शब्द और साहित्य की यह कहानी जब हम आज अपनी 21वीं सदी में पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि भले ही युग बदल गए हों लेकिन मनुष्य और साहित्य की यह परम्परा नहीं बदली है। आज भी मनुष्य जहां कहीं मनुष्य है वह साहित्य में ही बोल रहा है और कविता कहानी बनकर परिवर्तन और विकास की नई अवधारणाएं लिख रहा है। भाषा इसकी भिन्नता है लेकिन भाव इसकी एकता है। आदिम कबीलाई समाज, साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद, समाजवाद और अब लोकतंत्र इस मनुष्य के संघर्ष की ही अनुकृतियां है। विज्ञान, औद्योगिकरण, सूचना-प्रोद्योगिकी तथा बाजारवाद भी सभी इस समाज की प्रतिध्वनियां हैं। सत्य केवल यही है कि साहित्य में अनवरत समाज और समय की हलचल ही बोल रही है। लेकिन ज्ञान-विज्ञान के विस्तार ने आज मनुष्य को नई चुनौतियों और सपने बदल दिए हैं और ऐसे में साहित्य की धाराएं विचार और विवेक के नए क्षितिज तलाश कर रही हैं। समाज और समय के इस बदलते हुए चेहरे को पढ़कर अब हमें जरूरी लगता है कि ’ अतुल्य’ साहित्य में ही जीवित है। मेरा ऐसा अनुभव है कि जिस तरह देश और समाज के बुनियादी आधार संविधान से हटाए नहीं जा सकते उसी प्रकार साहित्य के मूल उद्देश्यों को भी मनुष्य को आकांक्षाओं से अलग नहीं किया जा सकता। वाद और विचारधाराएं भी सभी बदलती रही हैं लेकिन मनुष्य की मोक्ष और शांति केवल प्रकृति में ही निहित है। समाज और व्यवस्थाएं सभी इसके आवरण हैं तथा गरीबी-अमीरी, जाति, धर्म, लोकतंत्र और तानाशाही भी सब मनुष्य की चेतना के ही रंग हैं। इसलिए साहित्य में कालजयी शब्दों का वर्चस्व आज भी हमें मार्गदर्शन देता है।
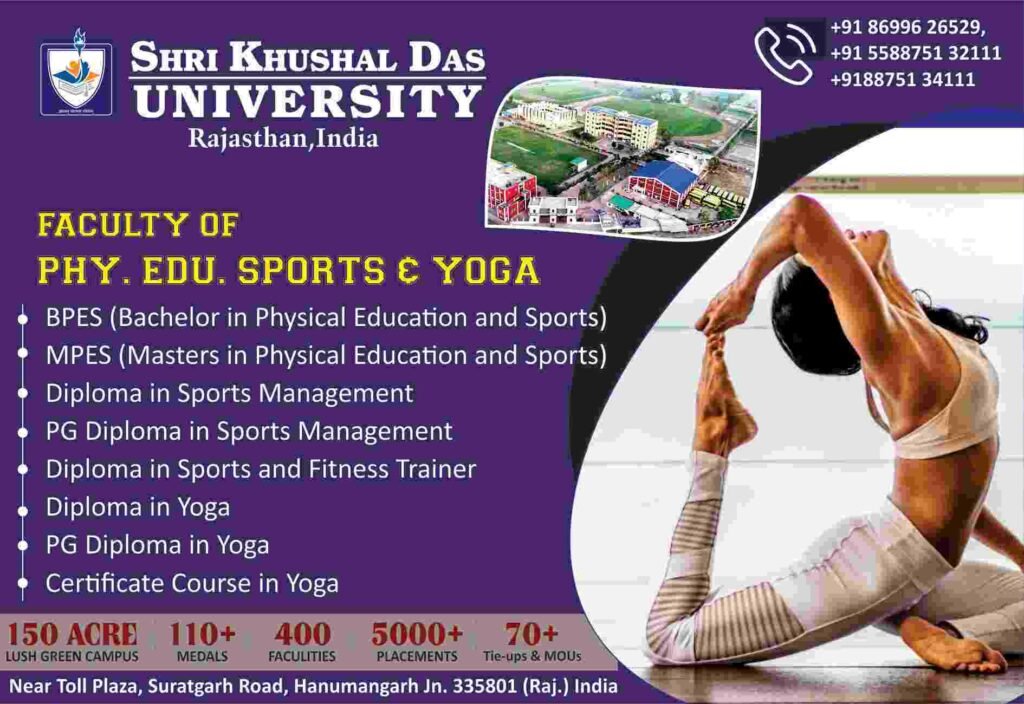
हम सब शब्द के उपासक लगातार इस विकल्प पर विचार करते रहते हैं कि शब्द की चेतना का अंतिम लक्ष्य क्या है और समय से मुठभेड़ करने में साहित्यकार की क्या भूमिका हो सकती है। मुझे ऐसा लगता है कि साहित्य में यदि कोई अनहदनाद है तो वह मनुष्य के लिए जगत कल्याण का ही है और युद्ध और शांति से लेकर समता और न्याय की खोज सभी संघर्ष पक्ष आखिरकार कलम के प्रत्येक सिपाही को एक प्रगतिशील चेतना से ही जोड़ते हैं और साहित्य को आत्मरंजन की अंधेरी सुरंग से बाहर निकाल कर समाज के व्यापक ’ बहुजन हिताय, बहुतन सुखायः’ के सरोकार तक ले जाते हैं। आपको याद होगा कि भारत के पहले मुक्ति संग्राम(1857) की सम्पूर्ण आधारभूत चेतना का निर्माण साहित्य के विचार और सामूहिक उद्घोष ने ही किया था। फिर 1947 की स्वंतत्रता का अभ्युदय भी साहित्य से ही अभिप्रेरित था तो 1961 के विदेशी आक्रमणों का प्रतिरोध भी साहित्य से ही निकला था। वंदेमातरम और जन-गण- मन जैसे गान साहित्य की देन हैं क्योंकि समय का इतिहास साहित्य में भी मनुष्य को ही दोहराता है। लेकिन हमारे नए भारत में लोकतंत्र की आकांक्षाओं का जो विप्लन अब आया है और ज्ञान-विज्ञान की खोज ने जिस बिखराव और भटकाव का तूफान मचाया है उससे यह भी तय होता जा रहा है कि साहित्य में समय के सभी भ्रम और यथार्थ टूट रहे हैं और विचारधराएं और उपभोक्ता बाजार की नई राजनीति हमारे समय में संघर्ष को बदल रही है।
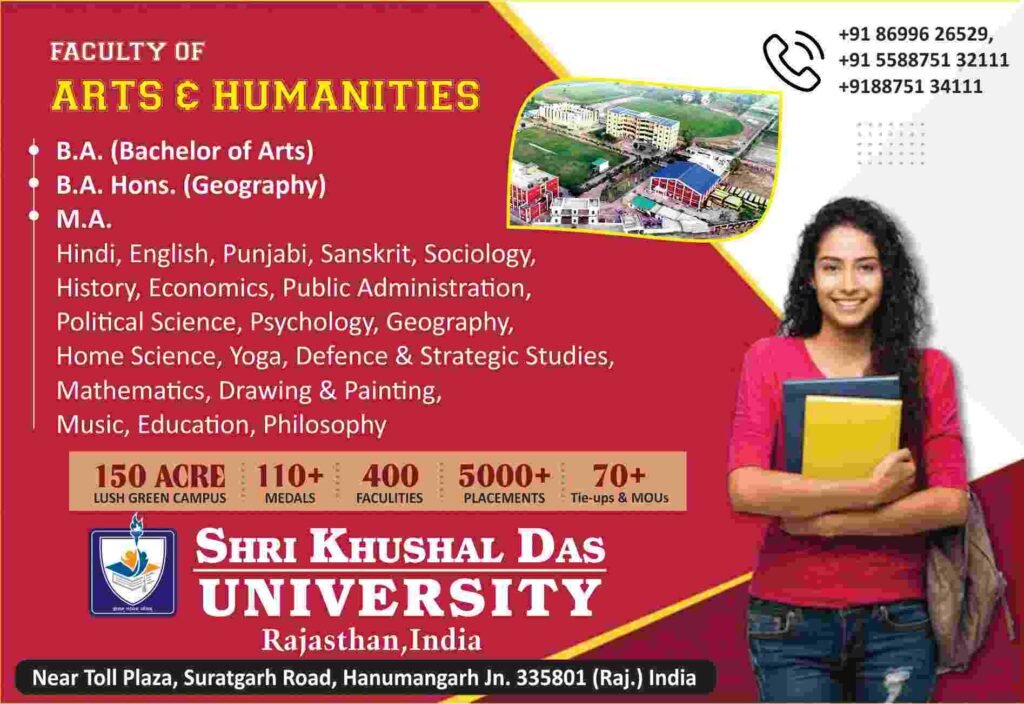
अब न कोई कबीर, न कोई कार्लमार्क्स, न कोई एडम स्मिथ और न कोई महात्मा गांधी हमारे बीच में है। हमारे पास केवल इतिहास में इनके शब्द हैं। मेरा मानना है कि मनुष्य की सभ्यता और संस्कृति का सच यदि आज भी कहीं सुरक्षित है तो वह अपने समय और समाज की साहित्य चेतना में ही किलकारियां मार रहा है। आज चेतना का यही प्रगतिशील स्वर, समाज की अंतर्धारा है और हम इसे अपने-अपने दायरे में अपने-अपने आग्रह और सीमाओं में लड़ रहे हैं। कोई सगुण-निर्गुण होकर तो कोई कलावादी-यथार्थवादी बनकर तो कोई नास्तिक-आस्तिक रहकर तो कोई संकीर्णतावादी, उदारवादी दर्शन-परम्पराओं में बंटकर समय, राष्ट्र और पूंजीवाद-समाजवाद के झंडे उठाकर चल रहे है। लेकिन साहित्यकार अपनी नियति को जानते हुए भी शब्द और समय की दिशा को बदलने की महाभारत जारी रखता है।
लेकिन आज के समय में साहित्य की सबसे बड़ी चुनौती बाजार से और विज्ञान के प्रयोग से आ रही है। पूरी शताब्दी सिद्धांतविहीन राजनीति, श्रमविहीन सम्पत्ति, विवेकहीन भोग-विलास, चरित्र विहीन शिक्षा, नैतिकता विहीन व्यापार, मानवीयता विहीन विज्ञान और त्याग विहीन पूजा के सात पापों में बदल गई है। अधकचरे लोग विचारधारा के अंत की और कविता के मृत्यु की घोषणाएं कर रहे हैं। किंतु एक सच्चा साहित्यकार सदैव इस ध्येय वाक्य को याद रखता है कि शब्द कभी मरते नहीं हैं और विचार कभी डरते नहीं है। सूचना-प्रौद्योगिकि कभी स्थाई नहीं रहती, लेकिन शब्द और कला संगीत की संस्कृति का अंतनार्द शाश्वत रहता है। मनुष्य पिट जाता है किंतु साहित्य में मनुष्य और समय की परम्परा निर्बाध चलती रहती है। वाचिक परम्परा से ही लिखित परम्परा का विकास होता है हम सब रचनाकार अपनी-अपनी व्याख्या के साथ एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को दुनिया को बदलना सिखाते रहते हैं। अतः हमारा मानना है कि साहित्य में बोलता हुआ समाज की अन्तर्द्वनि ही है और शब्द तथा विचार इसका रूपांतरण है। कोई राष्ट्र और राज्य साहित्य से अपने को खोजता है तथा आज भी सत्य के प्रयोग एकमात्र साधारण से साधारण लेखक ही करता है। शब्द ही व्यष्टि से समाष्टि बन जाता है और एक से अनेक और वर्तमान से भविष्य का पथ प्रदर्शक हो जाता है। भारत में भी समस्त भाषाओं की यह प्रगतिशील साहित्य परपंरा आज भी हमें यही कहती है कि आत्महीनता और आत्ममुग्धता साहित्य में चेतना की पहली शत्रु है क्योंकि शब्द (लेखक) को एक संत की तरह जीना पड़ता है और सुकरात से लेकर मीरांबाई तक विष का प्याला ही पीना पड़ता है।
(लेखक राजस्थान साहित्य अकादमी के पूर्व अध्यक्ष, साहित्य मनीषी व वरिष्ठ पत्रकार हैं)