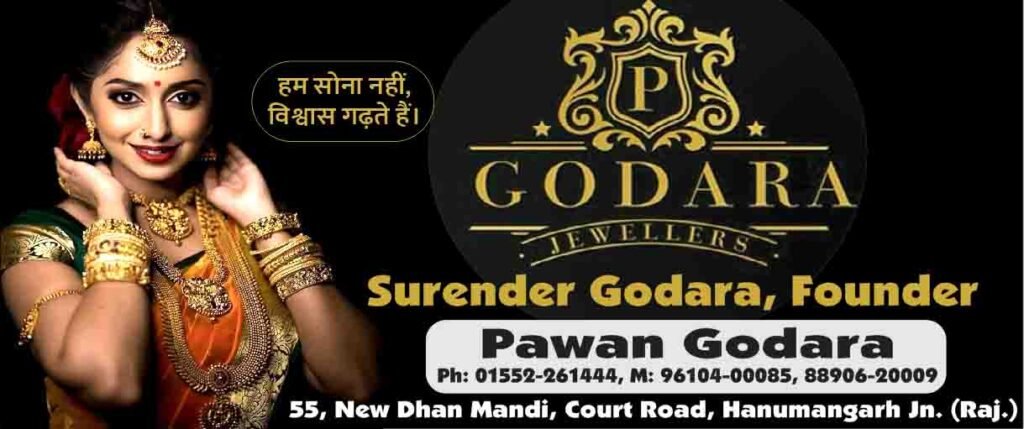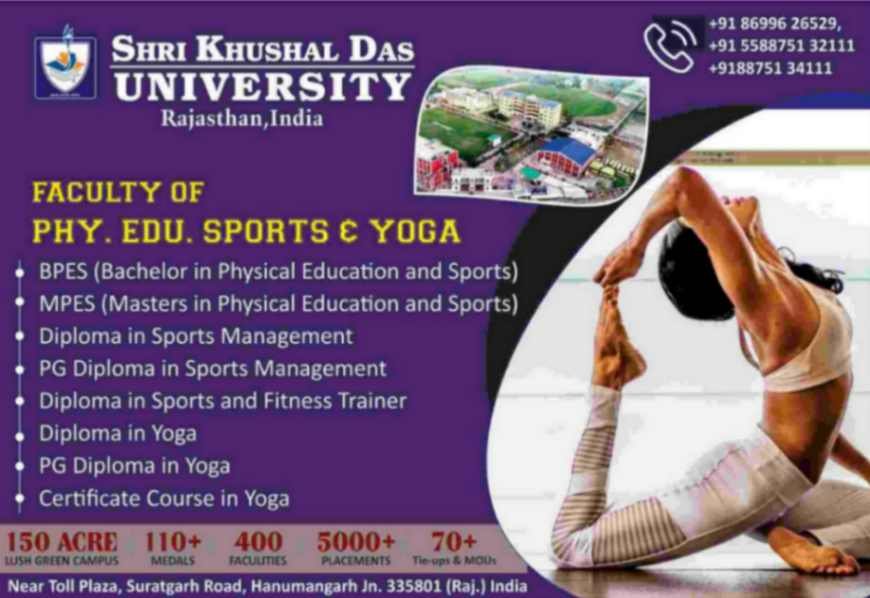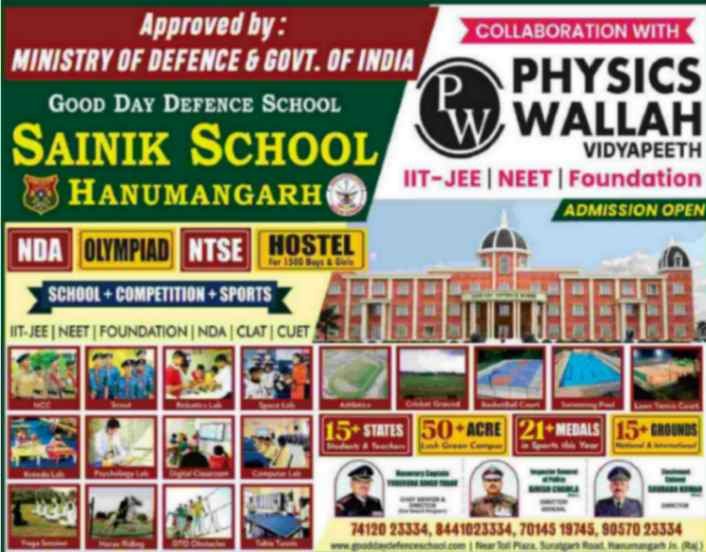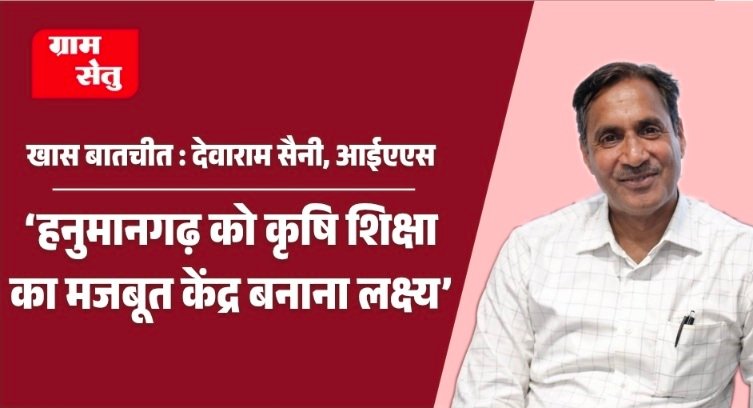अमित तिवारी.
कभी त्योहार कैलेंडर की तारीख नहीं होते थे, वे हमारे जीवन का सबसे जीवंत अहसास हुआ करते थे। उनके आने से पहले ही घर के आंगन में खुशियों की आहट सुनाई देने लगती थी। माँ रसोई में घंटों खड़ी होकर पकवान बनाती थी, पिता बाजार से नए कपड़े लाते थे और हम बच्चे उन थैलियों में झांक-झांक कर अपनी खुशियाँ ढूँढ़ते थे। त्योहार का मतलब सिर्फ एक दिन नहीं, बल्कि कई दिनों तक चलने वाली तैयारी और उत्साह होता था। वो समय था जब सफाई घर की कम और मन की ज्यादा होती थी। रिश्तों पर जमी धूल हटती थी, नाराज़गियाँ अपने आप ही खत्म हो जाती थीं।
दीवाली के दीयों की रोशनी दीवारों से ज्यादा दिलों को जगमगाती थी और होली का रंग चेहरों से ज्यादा रिश्तों पर चढ़ता था। मोहल्ले का हर घर अपना लगता था। बिना निमंत्रण के लोग एक-दूसरे के यहाँ पहुँच जाते थे और घंटों साथ बैठकर हँसते-बोलते थे।
त्योहारों का असली अर्थ ही था, अपनापन, मेल-मिलाप और साथ बिताए गए वे अनमोल पल। लेकिन अब त्योहार आते तो हैं, पर वह वो बेसब्री नहीं लाते। घर भी सजते हैं, पर आंगन सूना रहता है। मिठाइयाँ आती हैं, पर माँ के हाथों का स्वाद कहीं खो गया है।
अब शुभकामनाएँ दरवाज़े पर दस्तक नहीं देतीं, मोबाइल की स्क्रीन पर चमक जाती हैं। एक दूसरे से मिलने की जगह अब फॉरवर्ड मैसेज ने ले ली है। एक साथ बैठकर हँसने की परंपरा भी अब ‘ऑनलाइन’ हो गई है। संयुक्त परिवारों के बिखरने के साथ त्योहारों की रौनक भी जैसे अलग-अलग शहरों में बँट गई है। पहले मोहल्ले का हर घर अपना लगता था, अब अपने ही घर में सब अपने-अपने कमरों तक सीमित हो गए हैं। समय बचाने की दौड़ में हमने वे पल ही खो दिए, जो जीवन को रंगीन बनाते थे।
पर सच यह भी है कि त्योहारों की चमक कम नहीं हुई है, हमने उसे महसूस करना कम कर दिया है। अगर हम फिर से थोड़ी सी कोशिश करें, अपने हाथ से एक पकवान बना लें, किसी रूठे को मना लें, कुछ समय मोबाइल से दूर रहकर अपनों के साथ बैठ जाएँ, तो वही पुरानी रौनक लौट सकती है। क्योंकि त्योहार बाजार की चीज़ नहीं हैं, वे अपनेपन का अहसास हैं। और अपनेपन की रोशनी कभी फीकी नहीं पड़ती, बस हमें फिर से उसे महसूस करने की जरूरत है।