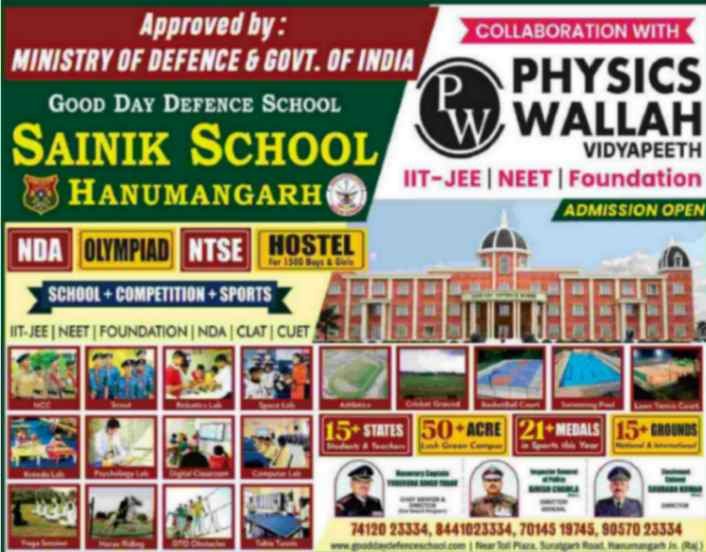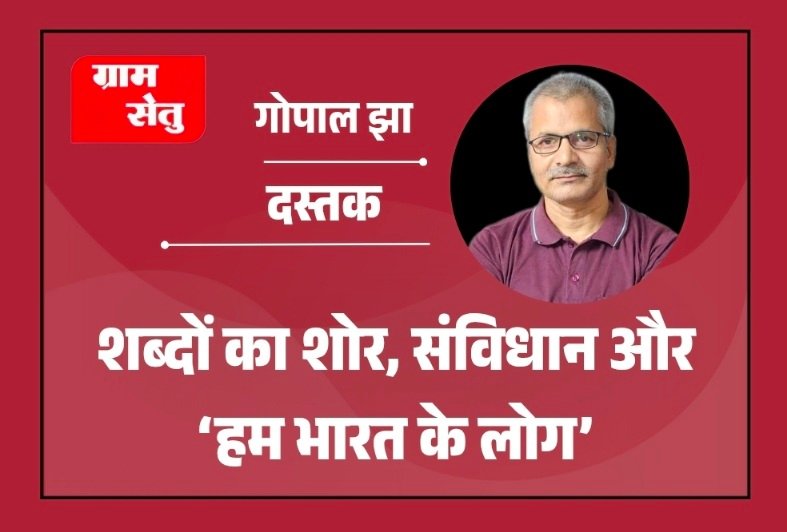




गोपाल झा
कॉलेज में अध्यापन का अपना ही आनंद है। क्लासरूम एक छोटी-सी दुनिया होती है, जहाँ किताबें बोलती हैं और सवाल करवटें लेते हैं। मैंने अपने अध्यापन के दिनों में एक आदत बना ली थी। हर पीरियड के अंत में दस मिनट का ‘प्रश्नकाल’। शर्त बस इतनी, जो पढ़ाया है, उसी पर सवाल होगा। मक़सद रटंत नहीं, समझ पैदा करना था।
एक दिन उसी प्रश्नकाल में एक छात्र ने ऐसा सवाल दागा कि मैं ठिठक गया। बोला, ‘सर, 15 अगस्त और 26 जनवरी हम लगभग एक जैसे ही मनाते हैं। पर दोनों में फर्क क्या है?’ सवाल सादा था, मगर उसकी तह में गहरी बेचैनी छुपी थी। मैंने बिना ज़्यादा सोचे कहा, ‘15 अगस्त हमें आज़ादी का एहसास कराता है, विदेशी गुलामी से मुक्ति का जश्न है। और 26 जनवरी हमें दायित्व का बोध कराता है।’ क्लास में ख़ामोशी छा गई। दरअसल, यही सच है। फर्क बस इतना ही है।
मगर असली सवाल यह है कि क्या हम, ‘हम भारत के लोग’, गणतंत्र दिवस मनाते वक्त इस दायित्व को याद रखते हैं? या फिर तिरंगा फहराकर, परेड देखकर और मिठाई खाकर अपनी ज़िम्मेदारी पूरी मान लेते हैं?
राजनीति पर नज़र डालिए तो जवाब खुद-ब-खुद सामने आ जाता है। राजनीति अब सेवा का ज़रिया नहीं रही। यह कड़वा सच है, मगर सच यही है। अब यह बाकायदा एक कारोबार बन चुकी है। टिकट पाने के लिए मोटी रकम, चुनाव जीतने के लिए करोड़ों का ख़र्च, यह सब निवेश की तरह देखा जाता है। और निवेश का उसूल सब जानते हैं, रिटर्न। जीतने के बाद वही पैसा चार गुना वसूलने की जुगत लगाई जाती है। इसके लिए क़ानून, कायदे, नैतिकता, सब ताक़ पर रख दिए जाते हैं। सेवा की बात भाषणों में रहती है, अमल में नहीं।
शासन और प्रशासन की भूमिका जनता को राहत देने की होती है। मगर कितने अफ़सर और कर्मचारी इस जज़्बे के साथ दफ़्तर आते हैं? अगर ऐसा होता, तो आए दिन रिश्वत लेते पकड़े जाने की ख़बरें सुर्खियां न बनतीं। फ़ाइलें जनता की हों तो धूल जम जाती है, दलाल की हों तो रफ़्तार पकड़ लेती हैं। यह व्यवस्था की बीमारी है, जो अब मामूली नहीं रही, पुराना मर्ज़ बन चुकी है।
न्यायपालिका की हालत पर क्या कहा जाए। वहाँ न्याय मानो चीख़-चीख़ कर फ़रियाद कर रहा हो, मगर सुनने वाला कोई नहीं। तारीख़ पर तारीख़, साल दर साल और आखिरकार, पीड़ित या तो टूट जाता है या दुनिया ही छोड़ देता है। इंसाफ़ अगर इतनी देर से मिले कि उसका मतलब ही ख़त्म हो जाए, तो वह इंसाफ़ नहीं, एक तसल्ली भर रह जाता है।
एक ज़माना था जब मीडिया को जनता की आवाज़ कहा जाता था। वह हुक्मरानों से सवाल करता था, हक़ीक़त सामने लाता था। आज वही मीडिया सत्ता की गिरफ़्त में क़ैद सा लगता है। सत्तापक्ष से सवाल पूछने की हिम्मत कम और विपक्ष को घेरने का शौक़ ज्यादा दिखता है। नतीजा यह कि विपक्ष भी बदनामी के डर से संघर्ष छोड़ता जा रहा है। लोकतंत्र में असहमति की जगह सिकुड़ती जा रही है।
और जनता? जनता को धर्म और जाति की ‘अफ़ीम’ चटा दी गई है। जब भी कोई होश में आने की कोशिश करता है, कोई नया मुद्दा उछाल दिया जाता है। लोग फिर पक्ष-विपक्ष में बँट जाते हैं और सियासतदान अगली चाल की तैयारी में लग जाते हैं, बेशर्म मुस्कान के साथ। राष्ट्रवाद, धर्म, जाति और भाषा ये सब वोटबैंक के हथियार बन चुके हैं। संविधान की बातें हर मंच पर होती हैं, मगर उसकी सुनवाई कहीं नहीं।
ऐसे में लगता है जैसे संविधान मौन खड़ा है, बेबस, लाचार। देशहित हाशिये पर है, शोर बस शब्दों का है। धर्म और राष्ट्र के नाम पर दोनों का नुकसान हो रहा है। लोग बँटते जा रहे हैं, और सियासतदानों के चेहरों पर रौनक बढ़ती जा रही है। जो राष्ट्रवाद का सबसे ऊँचा नारा लगाते हैं, वही विदेशी ताक़तों के सामने झुकते भी दिख जाते हैं। अफ़सोस, इस पर बोलने वाले गिनती के रह गए हैं।
गणतंत्र दिवस हमें याद दिलाता है कि हम सिर्फ़ वोटर नहीं, नागरिक हैं। वोट देने के बाद भी हमारी ज़िम्मेदारी ख़त्म नहीं होती। सरकार की हर बात पर हामी भरना नागरिक धर्म नहीं है। सवाल पूछना, आलोचना करना, जवाब माँगना, यही लोकतंत्र की रूह है। ‘अंधभक्त’ या ‘चमचा’ कहलाने से बेहतर है कि हम सच्चे भारतीय नागरिक बनें। यही गणतंत्र दिवस का असली मतलब है, अगर समझ में आए तो।
-लेखक भटनेर पोस्ट मीडिया ग्रुप के चीफ एडिटर हैं